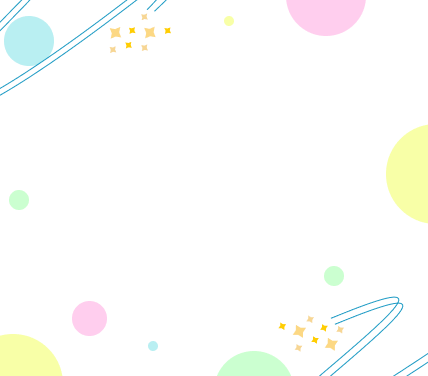Apvah Tantra Kya Hai: अपवाह तंत्र एक प्राकृतिक जल व्यवस्था है, जिसमें नदियाँ, छोटी नदियाँ, और तालाब जैसे पानी के स्रोत आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क ज़मीन के ऊपर बहने वाले पानी को एक निर्धारित दिशा में प्रवाहित करता है, जिससे जल का प्रवाह और वितरण सुचारू रूप से होता है। इस प्रक्रिया से एक जुड़ी हुई और संगठित जलवायु व्यवस्था बनती है, जिसे हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। इस ब्लॉग में आप अपवाह तंत्र क्या है? (Apvah Tantra Kya Hai), अपवाह तंत्र की महत्ता, इसके कार्यप्रणाली और इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे।
This Blog Includes:
- अपवाह तंत्र क्या है? (Apvah Tantra Kya Hai)
- भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र
- हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास
- हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उनके अपवाह तंत्र
- प्रायद्वीपीय नदी तंत्र
- नदी जल उपयोग की सीमाएं और चुनौतियाँ
- तटवर्ती नदियाँ
- अपवाह तंत्र के प्रकार
- अपवाह तंत्र के कार्य
- अपवाह तंत्र के खतरे
- अपवाह तंत्र की रक्षा
- अपवाह तंत्र के प्रतिरूप (Drainage Patterns)
- द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार (Dendritic Pattern or Trellis Pattern)
- आयताकार प्रतिरूप (Rectangular Pattern)
- जालीदार प्रतिरूप (Trellis Pattern)
- वलयाकार प्रतिरूप (Radial Pattern)
- कंटकीय या हुकनुमा प्रतिरूप (Barbed Pattern or Hook-shaped Pattern)
- अपकेन्द्रीय प्रतिरूप (Diverging Pattern)
- अभिकेन्द्री अरीय प्रतिरूप (Centripetal Radial Pattern)
- समान्तर प्रतिरूप (Parallel Pattern)
- अनिश्चित प्रतिरूप (Deranged Pattern)
- भूमिगत प्रतिरूप (Underground Pattern)
- पूर्ववर्ती प्रतिरूप (Antecedent Pattern)
- पूर्णरोपित प्रतिरूप या अध्यारोपित प्रतिरूप (Superimposed Pattern)
- अपवाह तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
- FAQs
अपवाह तंत्र क्या है? (Apvah Tantra Kya Hai)
अपवाह तंत्र वह प्रणाली है, जिसमें पानी एक निश्चित मार्ग से बहता है, जो नदियों, झीलों, नालों और अन्य जल निकायों का एक नेटवर्क है। यह तंत्र पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। भारत में कई प्रमुख अपवाह तंत्र हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कृष्णा नदियाँ। ये नदियाँ देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की आपूर्ति करती हैं और कृषि, उद्योग, और घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं।
अपवाह तंत्र का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह मिट्टी को पोषित करता है, जिससे पौधों और जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, अपवाह तंत्र बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जिससे बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हालांकि, अपवाह तंत्र प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रदूषण अपवाह तंत्र में पानी को दूषित कर सकता है, जिससे यह पीने, मछली पकड़ने और अन्य उपयोगों के लिए असुरक्षित हो जाता है।
भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र
भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं:
- हिमालय से निकलने वाली नदियाँ: ये नदियाँ बारहमासी होती हैं क्योंकि इन्हें बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से पानी मिलता है।
- दक्षिण क्षेत्र (प्रायद्वीपीय पठार) से निकलने वाली नदियाँ: इनमें से अधिकांश नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं और मौसमी होती हैं।
हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास
हिमालय पर्वतीय नदियों की उत्पत्ति पर भूवैज्ञानिकों के बीच विभिन्न दृष्टिकोण हैं। एक प्रमुख मान्यता यह है कि मायोसिन युग (लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व) में ‘शिवालिक’ या ‘इंडो-ब्रह्म’ नामक एक विशाल नदी हिमालय की लंबाई के समानांतर, असम से पंजाब तक बहती थी। यह नदी अंततः निचले पंजाब में सिंध की खाड़ी में मिलकर समाप्त होती थी। शिवालिक पहाड़ियों की निरंतर उपस्थिति, उनका झील जैसा उद्गम और जलोढ़ मिट्टी (जिसमें रेत, चिकनी मिट्टी, गोल पत्थर और कंकड़ शामिल हैं) से बने होने के कारण इस विचार को बल मिलता है।
मान्यता है कि समय के साथ इंडो-ब्रह्म नदी तीन प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई:
- पश्चिम में सिंधु और उसकी पाँच सहायक नदियाँ,
- मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ,
- पूर्व में ब्रह्मपुत्र और हिमालय से आने वाली उसकी सहायक नदियाँ।
यह विशाल नदी संभवतः प्लाइस्टोसिन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग और पोटवार पठार (दिल्ली रिज) के ऊपर उठने के कारण विभाजित हो गई। इस क्षेत्र ने सिंधु और गंगा जल निकासी प्रणालियों के बीच जलविभाजन का कार्य किया। इसी प्रकार, मध्य प्लाइस्टोसिन काल में राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच स्थित मालदा गैप के धंसने के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों की दिशा बदल गई और वे बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगीं।
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उनके अपवाह तंत्र
हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ और उनके अपवाह तंत्र निम्नलिखित हैं:
सिंधु तंत्र
सिंधु नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी घाटियों में से एक है, जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर (भारत में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर) के क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किमी (भारत में 1,114 किमी) है। यह नदी हिमालय की पश्चिमी नदियों में सबसे अधिक पश्चिम में स्थित है। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत में स्थित बोखर चू (Bokhar chu) हिमनद से होता है, जो 31°15′ उत्तर और 80°40′ पूर्व पर 4,164 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे “सिंगी खंबन” (Singi khamban) कहा जाता है, जिसका अर्थ है “शेर के मुख”।
यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर-पश्चिम दिशा से बहते हुए लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर पाकिस्तान के चिल्लास और दर्दिस्तान में प्रवेश करती है।
सिंधु नदी की सहायक नदियाँ
बाएं भाग में बहने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ:
- श्योक
- गिलगित
- जास्कर
- हुंजा
- नुब्रा
- शिगार
- गास्टिंग
- द्रास
इसके अलावा, अन्य सहायक नदियाँ जैसे खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हैं और मीठनकोट के पास पंजाब में पंजनाद में मिल जाती हैं।
पंजाब में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ:
- सतलुज
- व्यास
- रावी
- चेनाब
- झेलम
सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ का विवरण
- चेनाब: चेनाब नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनती है, जो हिमाचल प्रदेश में केलांग और तांडी संगम करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1,180 किलोमीटर बहती है।
- रावी: यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पश्चिम से निकलकर चम्बा घाटी से बहती है। यह नदी पीरपंजाल और धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है और चेनाब नदी में मिलती है।
- व्यास: व्यास नदी समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से होकर धौलाधर पर्वत से निकलकर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां सतलुज नदी में मिल जाती है।
- सतलुज: यह नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊँचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है और भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किमी तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है।
गंगा तंत्र
गंगा भारत की सबसे धार्मिक और सांस्कृतिक नदियों में से एक है। इसका जन्म उत्तराखंड के हिमालयी ग्लेशियरों से होता है और यह उत्तर भारत से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के कई सहायक नदियाँ हैं, जो इसे एक विशाल अपवाह तंत्र में बदल देती हैं।
गंगा का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा है, जो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें यमुना, सोन जैसी प्रमुख नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं:
- रामगंगा
- गोमती
- घाघरा
- गंडक
- कोसी
ब्रह्मपुत्र तंत्र
ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो औसत प्रवाह के मामले में पांचवें स्थान पर आती है। यह नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5,300 मीटर की ऊँचाई पर निकलती है। इसका जन्म तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे “सांग्पो” (Tsangpo) के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ‘शोधक’।
रालगोंग त्सांग्पो (Ralong Tsangpo) एक प्रमुख सहायक नदी है, जो मध्य हिमालय में नामचा बरवा (7,755 मीटर) के पास बहते हुए एक गहरा महाखड्ड बनाती है, जिसे सिशांग और दिहांग कहा जाता है। असम घाटी में यह नदी 750 किलोमीटर की यात्रा करती है। इनमें से सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, जो एक पूर्ववर्ती नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ:
- बूढ़ी दिहिंग
- धनसिरी
- सुबनसिरी
- कामेंग
- मानस
- संकोश
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में “जमुना नदी” कहा जाता है। यह नदी पहले तिस्ता नदी से, फिर पद्मा (गंगा) नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके सहायक नदियाँ बड़ी होती हैं, जो इसके बाढ़ के कारण बनती हैं।
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से बहुत पुराना है। इसका पता नदियों की प्रौढ़ावस्था और उनकी चौड़ी और उथली घाटियों से चलता है। पश्चिमी तट के पास स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियाँ जल-विभाजक का कार्य करती हैं। नर्मदा और तापी को छोड़कर, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।
प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं। वहीं, प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि ये एक निश्चित मार्ग पर बहती हैं, विसर्प (meander) नहीं बनातीं और ये बारहमासी नहीं होतीं। हालांकि, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद हैं, जो विसर्प बनाती हैं और इनमें जलवृद्धि (water flow) भी अधिक होती है।
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के विकास में प्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:
- पश्चिमी पार्श्व का धंसाव: प्रारंभिक टर्शियरी काल में प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे का धंसाव हुआ, जिससे जल विभाजक (watershed) की समरूपता भंग हुई और नदियों के प्रवाह की दिशा प्रभावित हुई। इस घटना के परिणामस्वरूप नदियाँ अपनी वर्तमान दिशा में बहने लगीं।
- उत्तरी भाग का अवनमन और भ्रंश: हिमालय के उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवनमन हुआ, जिससे भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। इन घाटियों में नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं, जो जलोढ़ निक्षेप की कमी को दर्शाती हैं।
- प्रायद्वीप का झुकाव: इसी अवधि में प्रायद्वीप का उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर झुकाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगीं।
प्रायद्वीपीय नदी तंत्र
प्रायद्वीपीय अपवाह में कई प्रमुख नदी तंत्र शामिल हैं। उनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:
महानदी
महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलकर ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और 47 प्रतिशत भाग ओडिशा में है।
गोदावरी
गोदावरी को “दक्षिण गंगा” के नाम से भी जाना जाता है। यह 1,465 किलोमीटर लंबी नदी है, जो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से बहती हैं। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में, 20 प्रतिशत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी भाग आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम के दक्षिण में इसके निचले भागों में भारी बाढ़ का खतरा रहता है।
प्रमुख सहायक नदियाँ:
- वैनगंगा
- इंद्रावती
- प्राणहिता
- मंजरा
कृष्णा
यह दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो महाबलेश्वर से बहती है। इसकी लंबाई 1,401 किलोमीटर है, और इसका जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र (27%), कर्नाटक (44%), और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (29%) में फैला हुआ है। इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं:
- कोयना
- तुंगभद्रा
- भीमा
कावेरी
कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडु में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका जलग्रहण क्षेत्र केरल (3%), कर्नाटक (41%), और तमिलनाडु (56%) में है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं:
- काबिनी
- भवानी
- अमरावती
नर्मदा
नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से 1,057 मीटर की ऊँचाई से निकलती है और 1,312 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। इसके मार्ग में महाखड्ड और जबलपुर के पास धुआँधार जल प्रपात स्थित हैं।
तापी
यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह बेतुल जिले में मुलताई से निकलती है और 724 किलोमीटर लंबी है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 79 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में, 15 प्रतिशत मध्य प्रदेश में, और 6 प्रतिशत गुजरात में है।
लूनी
लूनी नदी अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के पास दो धाराओं (सरस्वती और सागर्मी) से उत्पन्न होती है और बाद में लूनी के नाम से पहचानी जाती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, जो कच्छ के रण में जाकर मिलती है।
नदी जल उपयोग की सीमाएं और चुनौतियाँ
- जल का असमान प्रवाह
भारत की नदियाँ हर साल बहुत ज्यादा जल बहाती हैं। बारहमासी नदियाँ सालभर बहती हैं, लेकिन बाढ़ के समय पानी बढ़ जाता है और शुष्क मौसम में पानी कम हो जाता है। अधिकतर पानी बारिश के दौरान बाढ़ में बहकर समुद्र में मिल जाता है। इस दौरान कुछ हिस्सों में सूखा पड़ जाता है। यह समस्या जल की कमी या इसके प्रबंधन की हो सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए जल भंडारण, बेहतर जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय किए जा सकते हैं। - नदियों को जोड़ने का विचार
क्या जल का अधिक हिस्सा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से यह समस्या हल हो सकती है? हमारे देश में नदियों को जोड़ने की योजना पर चर्चा हो रही है। हालांकि, गंगा का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित करना मुश्किल है क्योंकि जमीन की ऊबड़-खाबड़ प्रकृति और पानी उठाने की समस्या है। यह भी सोचना जरूरी है कि उत्तर भारत में क्या इतना अतिरिक्त पानी है जिसे स्थायी रूप से भेजा जा सके। - नदी जल उपयोग से जुड़ी समस्याएँ
नदी जल उपयोग से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याएँ हैं:- जल की कमी
- नदी जल का प्रदूषण
- नदी में गाद का जमा होना
- जल का असमान प्रवाह
- राज्यों के बीच जल विवाद
- बस्तियाँ नदी के किनारे बढ़ने से नदी की सिकुड़ती हुई धाराएँ
- जल की कमी
- नदी जल प्रदूषण
नदियाँ कई कारणों से प्रदूषित होती हैं:
- शहरों का गंदा पानी नदियों में गिरता है।
- उद्योगों का कचरा भी नदियों में डाला जाता है।
- श्मशान घाटों से मृत शरीरों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।
- कुछ त्योहारों में फूल और मूर्तियाँ नदियों में डाली जाती हैं।
- स्नान और कपड़े धोने से भी जल प्रदूषित होता है।
- शहरों का गंदा पानी नदियों में गिरता है।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस योजनाओं की जरूरत है। गंगा एक्शन प्लान और यमुना सफाई अभियान जैसे प्रयास इस दिशा में किए गए हैं। इन योजनाओं पर और सामग्री जुटाकर एक विस्तृत लेख तैयार किया जा सकता है।
तटवर्ती नदियाँ
भारत में कई छोटी तटवर्ती नदियाँ हैं। पूर्वी तट के डेल्टा में समुद्र में मिलन वाली नदियाँ कम हैं, जबकि पश्चिमी तट पर लगभग 600 ऐसी नदियाँ हैं। राजस्थान में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो समुद्र में नहीं मिलतीं; ये खारे झीलों में समाप्त हो जाती हैं और रेत में लुप्त हो जाती हैं। इन नदियों की समुद्र में कोई निकासी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, कुछ मरुस्थलीय नदियाँ भी होती हैं, जो कुछ दूरी तक बहने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, लूनी, मच्छ, स्पेन, सरस्वती, बनास और घग्गर जैसी नदियाँ शामिल हैं।
अपवाह तंत्र के प्रकार
अपवाह तंत्र को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- अस्थायी अपवाह तंत्र: ये तंत्र केवल बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं और पानी बहते हैं।
- स्थायी अपवाह तंत्र: ये तंत्र पूरे वर्ष जल प्रवाहित करते हैं।
- अंतर्देशीय अपवाह तंत्र: ये समुद्र में नहीं बहते, बल्कि अंतर्देशीय झीलों, नमक दलदलों या भूमिगत जल में समाप्त होते हैं।
- बाह्य अपवाह तंत्र: ये तंत्र समुद्र में गिरते हैं और वहां जल का अंत होता है।
अपवाह तंत्र के कार्य
अपवाह तंत्र के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं:
- पानी की आपूर्ति: ये तंत्र पीने, सिंचाई, उद्योग और अन्य आवश्यकताओं के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं।
- मिट्टी की पोषण: अपवाह तंत्र मिट्टी को पोषित करते हैं, जो पौधों और जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक है।
- बाढ़ नियंत्रण: ये तंत्र बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य: अपवाह तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए आवश्यक है।
अपवाह तंत्र के खतरे
अपवाह तंत्र को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से कई खतरे हो सकते हैं:
- प्रदूषण: अपवाह तंत्र में प्रदूषित जल का समावेश हो सकता है, जिससे यह पीने, मछली पकड़ने और अन्य उपयोगों के लिए असुरक्षित हो जाता है।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखा जैसी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जो अपवाह तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं।
अपवाह तंत्र की रक्षा
अपवाह तंत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि हम पानी की आपूर्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की रक्षा कर सकें। इसके लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- प्रदूषण से बचाव: अपवाह तंत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाना।
- जलवायु परिवर्तन से निपटना: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उपायों को लागू करना।
- पानी का जिम्मेदारी से उपयोग: पानी का सही और संतुलित उपयोग करना।
अपवाह तंत्र के प्रतिरूप (Drainage Patterns)
अपवाह तंत्र में नदियों और उनकी सहायक धाराओं का ज्यामितीय विन्यास (geometrical arrangement) तथा इस विन्यास से निर्मित विशिष्ट आकार या खाका अपवाह प्रतिरूप (drainage pattern) कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र की मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जिस प्रकार की आकृति बनाती हैं, उसे ही अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यह प्रतिरूप उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना (geological structure), ढाल (slope) और चट्टानों के प्रकार (rock types) पर निर्भर करता है।
विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिस्थितियों और स्थलाकृति के कारण, अपवाह तंत्र कई अलग-अलग प्रकार के प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रमुख अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित हैं:
द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार (Dendritic Pattern or Trellis Pattern)
- इस प्रतिरूप में नदियाँ और उनकी सहायक धाराएँ एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैलती हुई दिखाई देती हैं। मुख्य नदी एक तने के समान होती है, और सहायक नदियाँ उससे विभिन्न कोणों पर जुड़ती हुई शाखाओं का रूप लेती हैं।
- यह प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ चट्टानें एक समान कठोरता वाली होती हैं और उनमें कोई विशेष संरचनात्मक नियंत्रण (structural control) नहीं होता है। धरातल का ढाल भी अपेक्षाकृत एक समान होता है।
- उत्तरी मैदान की अधिकांश नदियाँ, विशेषकर गंगा नदी तंत्र, इस प्रकार का प्रतिरूप दर्शाती हैं।
आयताकार प्रतिरूप (Rectangular Pattern)
- इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ समकोण (right angles) पर मिलती हैं, जिससे एक आयताकार या जालीदार संरचना बनती है।
- यह प्रतिरूप उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ चट्टानों में कठोरता में अंतर होता है और उनमें भ्रंश (faults) या संधियाँ (joints) विकसित होती हैं। नदियाँ इन कमजोर क्षेत्रों का अनुसरण करती हैं और समकोण पर मुड़ती हैं।
- विंध्य पर्वतमाला और छोटा नागपुर पठार के कुछ हिस्सों में इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है।
जालीदार प्रतिरूप (Trellis Pattern)
- इस प्रतिरूप में मुख्य नदियाँ समानांतर रूप से बहती हैं और छोटी सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर जुड़ती हैं। यह प्रतिरूप एक जाली या सीढ़ी की तरह दिखाई देता है।
- यह प्रतिरूप वलित पर्वतीय क्षेत्रों (folded mountainous regions) में विकसित होता है, जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। मुख्य नदियाँ लंबी घाटियों (valleys) का अनुसरण करती हैं, जबकि सहायक नदियाँ कठोर चट्टानों को काटकर समकोण पर उनसे मिलती हैं।
- हिमालय के निचले क्षेत्रों और पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में इस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है।
वलयाकार प्रतिरूप (Radial Pattern)
- इस प्रतिरूप में नदियाँ एक केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से चारों दिशाओं में बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। यह प्रतिरूप एक पहिये की तीलियों जैसा दिखता है।
- यह प्रतिरूप ज्वालामुखी शंकुओं (volcanic cones), गुंबदाकार पर्वतों (domed mountains) या उत्थित पठारों (uplifted plateaus) पर विकसित होता है।
- अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और रांची पठार पर इस प्रकार का प्रतिरूप देखा जा सकता है।
कंटकीय या हुकनुमा प्रतिरूप (Barbed Pattern or Hook-shaped Pattern)
- इस प्रतिरूप में सहायक नदियाँ मुख्य नदी से विपरीत दिशा में मुड़कर मिलती हैं, जिससे एक कांटे या हुक जैसी आकृति बनती है।
- यह प्रतिरूप नदी अपहरण (river capture) के कारण विकसित होता है। जब एक तीव्र गति से बहने वाली नदी धीमी गति से बहने वाली नदी के ऊपरी मार्ग को काट लेती है और उसका पानी अपने में मिला लेती है, तो अपहृत नदी की सहायक धाराएँ मुख्य नदी से विपरीत दिशा में मुड़कर मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
- भारत में कुछ स्थानों पर नदी अपहरण के कारण इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है।
अपकेन्द्रीय प्रतिरूप (Diverging Pattern)
- यह वलयाकार प्रतिरूप के समान होता है, जिसमें नदियाँ एक केंद्रीय बिंदु से विभिन्न दिशाओं में बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं।
- यह प्रतिरूप भी गुंबदाकार संरचनाओं या ऊँचे क्षेत्रों पर विकसित होता है जहाँ से पानी चारों ओर फैलता है।
- वलयाकार प्रतिरूप में एक स्पष्ट केंद्रीय शिखर होता है, जबकि अपकेन्द्रीय प्रतिरूप में एक विस्तृत उच्च भूमि हो सकती है जिससे नदियाँ निकलती हैं।
अभिकेन्द्री अरीय प्रतिरूप (Centripetal Radial Pattern)
- यह अपकेन्द्रीय प्रतिरूप के विपरीत होता है। इस प्रतिरूप में विभिन्न दिशाओं से नदियाँ आकर एक केंद्रीय गर्त (central depression), झील या दलदल में मिलती हैं।
- यह प्रतिरूप आंतरिक जल निकासी वाले क्षेत्रों (areas with inland drainage) में विकसित होता है, जहाँ नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है।
- राजस्थान की कुछ आंतरिक जल निकासी वाली नदियाँ सांभर झील में मिलकर इस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं।
समान्तर प्रतिरूप (Parallel Pattern)
- इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ एक-दूसरे के समानांतर बहती हैं।
- यह प्रतिरूप तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों या लंबी संकरी घाटियों में विकसित होता है, जहाँ नदियों को बहने के लिए सीमित स्थान मिलता है। यह भ्रंशों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में भी विकसित हो सकता है।
- पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर बहने वाली कुछ नदियाँ इस प्रकार का प्रतिरूप दर्शाती हैं।
अनिश्चित प्रतिरूप (Deranged Pattern)
- इस प्रतिरूप में नदियों का कोई निश्चित क्रम या दिशा नहीं होती है। नदियाँ आपस में अनियमित रूप से मिलती हैं, झीलें और दलदल पाए जाते हैं, और जलमार्ग अस्पष्ट होते हैं।
- यह प्रतिरूप हिमानी अपरदन (glacial erosion) वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जहाँ हिमनदों ने धरातल को अनियमित बना दिया है। पिघलते हुए बर्फ का पानी विभिन्न गड्ढों और निम्न भूभागों में भर जाता है और अनियमित जलमार्ग बनाता है।
- उत्तरी कनाडा और स्कैंडिनेविया के हिमानीकृत क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रतिरूप आम है।
भूमिगत प्रतिरूप (Underground Pattern)
- इस प्रतिरूप में नदियाँ धरातल के नीचे बहती हैं और सतह पर इनका कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता है।
- यह प्रतिरूप चूना पत्थर (limestone) जैसे घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। पानी चट्टानों में घुल जाता है और भूमिगत गुफाएँ और जलमार्ग बनाता है।
- भारत में मेघालय और बस्तर के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है।
पूर्ववर्ती प्रतिरूप (Antecedent Pattern)
- यह एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप है जो भूगर्भिक उत्थान (geological uplift) की प्रक्रिया से पहले से मौजूद था। जब भूमि का उत्थान होता है, तो नदी अपनी पुरानी घाटी को काटती रहती है और अपने मार्ग को बनाए रखती है, भले ही भूभाग की ढाल बदल जाए।
- इस प्रकार की नदियाँ अक्सर गहरी और संकरी घाटियाँ (gorges) बनाती हैं क्योंकि वे उत्थानित भूभाग को काटती हैं।
- सिंधु नदी और सतलज नदी हिमालय के उत्थान के बावजूद अपनी पुरानी घाटियों में बहती हैं और पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
पूर्णरोपित प्रतिरूप या अध्यारोपित प्रतिरूप (Superimposed Pattern)
- यह एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप है जो ऊपरी चट्टानी परतों पर विकसित होता है और बाद में नीचे की भूवैज्ञानिक संरचना पर अध्यारोपित हो जाता है, भले ही नीचे की संरचना ऊपरी संरचना से भिन्न हो।
- यह तब होता है जब एक क्षेत्र में पहले से मौजूद अपवाह तंत्र किसी नई भूवैज्ञानिक संरचना के ऊपर से बहता है जो बाद में उजागर हो जाती है। नदी अपने पहले के मार्ग को बनाए रखती है और नीचे की संरचना के अनुरूप समायोजित नहीं होती है।
- अध्यारोपित नदियाँ उन भूवैज्ञानिक संरचनाओं को भी काट सकती हैं जो उनके वर्तमान मार्ग के लिए अनुकूल नहीं हैं।
- छोटा नागपुर पठार की कुछ नदियाँ, जैसे कि दामोदर नदी, अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण मानी जाती हैं।
अपवाह तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
1. नदी द्रोणी और जल सांभर में क्या अंतर है?
उत्तर: जल सग्रहण क्षेत्र, जिसमें बड़ी नदियाँ बहती हैं और जो बड़े आकार का होता है, उसे नदी द्रोणी कहा जाता है। इसके विपरीत, अपवाहित क्षेत्र, जो छोटे नदी नालों की वजह से पानी नहीं बहा पाते क्योंकि उनका आकार छोटा होता है, उसे जल सांभर कहा जाता है।
2. वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रारूप क्या होते हैं?
उत्तर:
- वृक्षाकार अपवाह प्रारूप एक हल्की ढलान और समतल जमीन पर विकसित होता है, जिसमें मुख्य धारा से शाखाएँ बाहर की ओर फैलती हैं, जैसे एक पेड़ की शाखाएँ।
- जालीनुमा अपवाह प्रारूप एक ग्रिड या जाल जैसा दिखता है। यह तब विकसित होता है जब विभिन्न भूगर्भीय विशेषताएँ नदियों की दिशा को प्रभावित करती हैं।
3. अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रिया अपवाह प्रारूप में क्या अंतर है?
उत्तर: अपकेंद्रीय अपवाह प्रारूप तब बनता है जब नदियाँ पर्वत से अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं जबकि अभिकेंद्रिया अपवाह प्रारूप में नदियाँ चारों ओर से बहकर किसी गर्त या झील में मिल जाती हैं।
4. डेल्टा और ज्वरनदमुख में क्या अंतर होता है?
उत्तर:
- ज्वारनदमुख (estuaries) वे स्थान होते हैं जहां दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं और समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं। ज्वारनदमुखों का आकार ज्वारीय धाराओं और लहरों से बनता है।
- डेल्टा (delta) विशेष रूप से उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, और इनका आकार तलछट जमाव और नदी की गतिशीलता से बनता है।
FAQs
अपवाह तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा जल निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। इन वाहिकाओं के जाल को ‘अपवाह तंत्र’ कहा जाता है।
भारत में अपवाह तंत्र दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
दक्षिण क्षेत्र (प्रायद्वीपीय पठार) से निकलने वाली नदियाँ।
अपवाह या धरातलीय अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए पानी की धाराओं के रूप में नालों और नदियों में बहती है।
अपवाह तंत्र को इंग्लिश में Drainage System कहते हैं।
द्रोणी या जलसंभर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां बारिश या पिघली हुई बर्फ़ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है।
गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है।
अपवाह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर प्रवाहित करती हैं।
डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा अपने पानी और तलछट को किसी अन्य जल निकाय में खाली करने से होता है।
नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है।
गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है।
नर्मदा नदी एस्टुएरी बनाती है।
उम्मीद है आपको अपवाह तंत्र क्या है? (Apvah Tantra Kya Hai) के संदर्भ में हमारा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। UPSC और सामान्य ज्ञान से जुड़े ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ जुड़े रहें।

 One app for all your study abroad needs
One app for all your study abroad needs
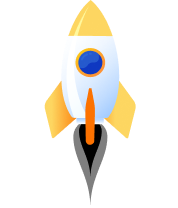


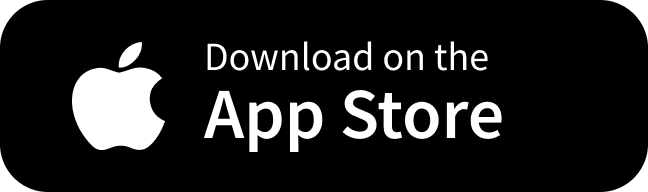











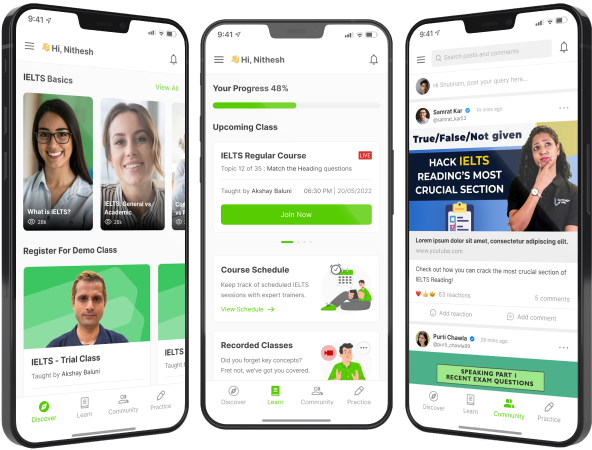



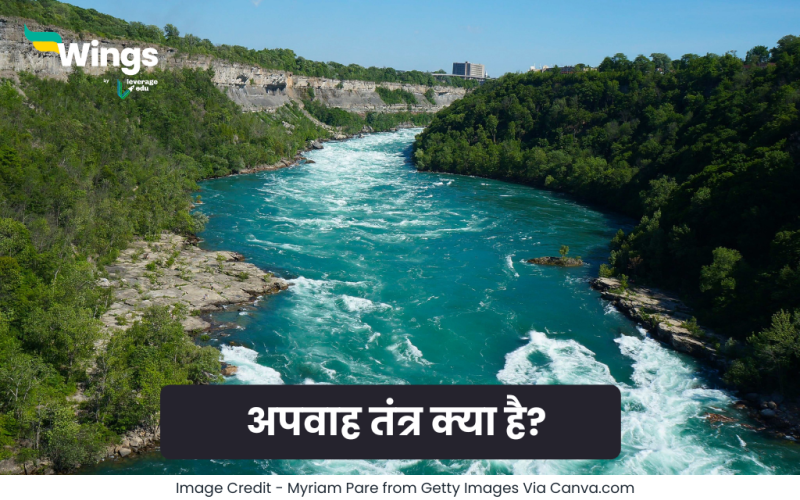

 45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!
45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!