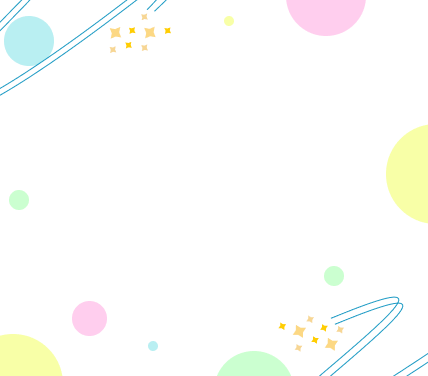Sansad Kya Hai: भारत का लोकतंत्र अपनी मज़बूत और संगठित संसदीय प्रणाली पर टिका हुआ है, जहां संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय होती है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और वित्तीय मामलों की निगरानी करना है। यह राष्ट्रपति और दो सदनों – राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (जन प्रतिनिधियों का सदन) – से मिलकर बनती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि संसद क्या है?, इसका ऐतिहासिक विकास कैसा रहा है, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली क्या है, तो यह ब्लॉग आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। यहां आपको संसद से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से मिलेगी, जो न केवल आपकी समझ को गहरा करेगी बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार होगी।
| विषय | विवरण |
| संस्था का नाम | भारतीय संसद |
| संसद के दो सदन | लोकसभा (संसद की संख्या: 545) और राज्यसभा (संसद की संख्या: 245) |
| निर्वाचन प्रक्रिया | लोकसभा: प्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा: अप्रत्यक्ष चुनाव |
| कार्य | कानून बनाना, सरकारी नीतियों की समीक्षा, जनहित पर विचार |
| महत्व | लोकतंत्र की रक्षा, जनहित में निर्णय लेना |
This Blog Includes:
संसद क्या है?
संसद किसी भी लोकतांत्रिक देश की मुख्य विधायिका (Legislature) होती है। यह एक ऐसा संस्थान है, जो कानून बनाने, सार्वजनिक नीति निर्धारण करने और सरकार की कार्यप्रणाली की निगरानी रखने का कार्य करता है। भारत में संसद दो सदनों से मिलकर बनती है – लोकसभा (जन प्रतिनिधियों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)।
संसद का इतिहास
भारत में संसद की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। ब्रिटिश संसद ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए एक संरचना तैयार की थी, जिसे भारतीय विधान परिषद (Indian Legislative Council) के नाम से जाना जाता था। यह परिषद 1861 में गठित की गई थी और इसे धीरे-धीरे और विस्तार दिया गया।
भारतीय संसद की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इसके बाद, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, भारत में एक विधायी परिषद की स्थापना की गई। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत एक द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान सभा ने देश के संविधान का मसौदा तैयार किया। 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया और भारतीय संसद का गठन हुआ। पहली लोक सभा का गठन 1952 में हुआ।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद का गठन
भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा ने संसद की संरचना को परिभाषित किया, जिसमें दो सदन—लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो विधायी कार्यों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
संसद की संरचना
भारतीय संसद दो सदनों में विभाजित है:
- लोकसभा (Lower House / जन प्रतिनिधि सभा) – यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण सदन है, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा सरकार बनाने और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- राज्यसभा (Upper House / राज्यों की परिषद) – इसे परिषद-ए-राज्य भी कहा जाता है। इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा निर्वाचित या नामांकित किए जाते हैं। यह सदन कानून निर्माण की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने और राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है।
यह द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameral System) भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और स्थिरता को बनाए रखने में सहायक है, जिससे विधायी प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बनती हैं।
लोकसभा की संरचना
भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की संरचना इस प्रकार है:
- लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं।
- इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
- लोकसभा के सदस्यों को आमतौर पर सांसद (MP – Member of Parliament) कहा जाता है।
- लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जो आम चुनावों के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होता है।
- भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी भंग कर सकते हैं।
लोकसभा की संरचना से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें
- लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा इस तरह किया जाता है कि हर राज्य को मिली सीटों की संख्या और उसकी जनसंख्या का अनुपात संतुलित हो।
- पहले, लोकसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, जो एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे।
- 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत, जनवरी 2020 में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए नामित सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी
- लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) –
- लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करने और उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं।
- लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करने और उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- लोकसभा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) –
- उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
- वर्तमान में, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है।
- उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
- कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) –
- जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सांसद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।
- इसका कार्य नए अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही को संचालित करना होता है।
- जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सांसद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।
लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि यह सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है और देश की नीतियों एवं कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
राज्यसभा की संरचना
राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो भारत के संघात्मक शासन का प्रतीक है। इसकी स्थापना संघीय इकाइयों (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से की गई थी।
- राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
- इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं।
- 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं।
- वर्तमान में, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं।
- राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
- इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे सदन की निरंतरता बनी रहती है।
राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं:
- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 30 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए।
- संविधान और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं का पालन करना चाहिए।
राज्यसभा की शक्तियां
हालांकि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की तुलना में सीमित हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:
- विधेयक पारित करना –
- कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित किए बिना कानून नहीं बन सकता।
- हालांकि, लोकसभा के पास विधेयकों को पारित करने की अधिक शक्ति होती है।
- वित्तीय मामलों में भूमिका –
- राज्यसभा को वित्तीय मामलों में सीमित अधिकार होते हैं।
- वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और पारित होने के बाद ही राज्यसभा में भेजा जाता है।
- राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे रोक नहीं सकती।
- संयुक्त बैठक का अधिकार –
- यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
- इस संयुक्त बैठक में लोकसभा का बहुमत अधिक होने के कारण निर्णय का अंतिम अधिकार लोकसभा के पास होता है।
राज्यसभा के पदाधिकारी
राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:
- सभापति (Chairman) –
- भारत के उपराष्ट्रपति पदेन (Ex-officio) राज्यसभा के सभापति होते हैं।
- वे सदन की कार्यवाही का संचालन और अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- उपसभापति (Deputy Chairman) –
- राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- वह सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
राज्यसभा संघीय संरचना की रक्षा और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीतियों की समीक्षा करने और विशेषज्ञता प्रदान करने वाला सदन है, जो भारत के विधायी ढांचे को संतुलित बनाता है।
संसद के कार्य
भारतीय संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य कानून बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली की निगरानी करना, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना और जनता की समस्याओं को उठाना है। इसके कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है:
1. विधायी (Legislative) कार्य
- नए कानूनों का निर्माण और पुराने कानूनों में संशोधन करना।
- संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को संचालित करना।
2. कार्यपालिका पर नियंत्रण (Executive Oversight)
- सरकार की नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करना।
- सरकार को जवाबदेह ठहराना और उसकी कार्यप्रणाली की निगरानी रखना।
- सार्वजनिक नीतियों की समीक्षा और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना।
- सार्वजनिक खातों की जांच और सरकारी खर्चों का लेखा-जोखा रखना।
3. वित्तीय (Financial) कार्य
- देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण और बजट पारित करना।
- कर निर्धारण और राजस्व संग्रह से संबंधित कानून बनाना।
- सरकार के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना और ऑडिट करना।
4. प्रशासनिक (Administrative) कार्य
- राष्ट्रपति का चुनाव और उनके कार्यों की निगरानी करना।
- सरकार के मंत्रियों का चयन और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना।
5. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्य
- राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण और देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना।
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौतों और संधियों को स्वीकृति देना।
- देश के रक्षा क्षेत्र, विदेशी मामलों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीतियां बनाना।
6. सामाजिक और जनहित कार्य
- नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना।
- देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना।
- लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाना और उनका समाधान निकालना।
संसद का महत्व
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ उठाते हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं। संसद का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार अपनी नीतियों और फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखे।
संसद देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, जहां विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों का निर्माण करते हैं। संसद के दो सदन— लोकसभा और राज्यसभा—अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ निभाते हैं।
- लोकसभा: जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों का सदन, जो जनता के विचारों और मुद्दों को संसद तक पहुँचाता है।
- राज्यसभा: राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, जो संघीय संरचना को मजबूत करता है और राज्यों के हितों की रक्षा करता है।
भारतीय संसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, जो नीतियों, विधानों और प्रशासनिक कार्यों को संतुलित और प्रभावी रूप से संचालित करने में मदद करती है।
संसद की भूमिका
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसकी भूमिका कई तरह की होती है:
- कानून बनाना
- वित्तीय नियंत्रण
- सरकार की निगरानी
- जनता की समस्याओं को उठाना
- राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना
- संविधान में संशोधन करना
- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना
जनहित के मामलों में संसद का प्रभाव
संसद न केवल कानून पारित करने का कार्य करती है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करती है। संसद में जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक बहस होती है, जिससे नीतिगत सुधार और समग्र विकास के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।
यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो देश के विकास, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। इसके माध्यम से नागरिकों की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, और संसद जनकल्याणकारी कानूनों का निर्माण करती है। भारतीय संसद की द्विसदनीय संरचना और इसकी कार्यप्रणाली लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। एक सुदृढ़ और प्रभावी संसद ही देश के उज्जवल भविष्य का आधार बन सकती है।
FAQs
भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा (जनप्रतिनिधियों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों का सदन) शामिल हैं। यह भारतीय लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है।
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद का सदस्य कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
संसद को “भारतीय संसद” या “संसद भवन” भी कहा जाता है।
संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार को जवाबदेह ठहराना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना और देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना है।
संसद के दो सदन होते हैं – राज्यसभा और लोकसभा।
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। संसद देश की विधायिका है और शासन संचालन की ज़िम्मेदारी निभाती है।
संविधान के अनुसार, संसद में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है।
संसद की अधिकतम स्वीकृत सदस्य संख्या लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञों के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।
सांसद (MP – Member of Parliament) संसद के सदस्य होते हैं और लोकसभा या राज्यसभा में कार्यरत होते हैं। विधायक (MLA – Member of Legislative Assembly) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। हर लोकसभा सदस्य (MP) के अंतर्गत 7 से 9 विधायक (MLA) हो सकते हैं।
आशा है, आपको संसद क्या है? (Sansad Kya Hai) से जुड़ी जरूरी जानकारियां यहां मिल गई होंगी। UPSC स्टडी मटेरियल से जुड़े ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

 One app for all your study abroad needs
One app for all your study abroad needs
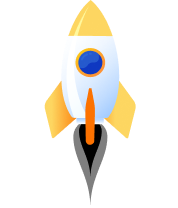


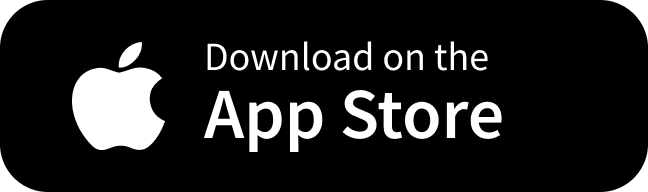











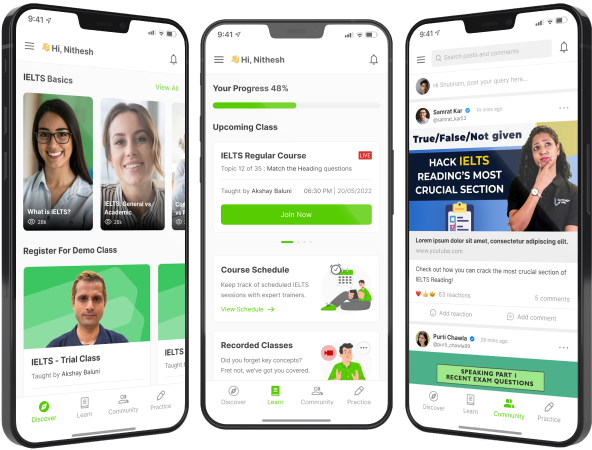



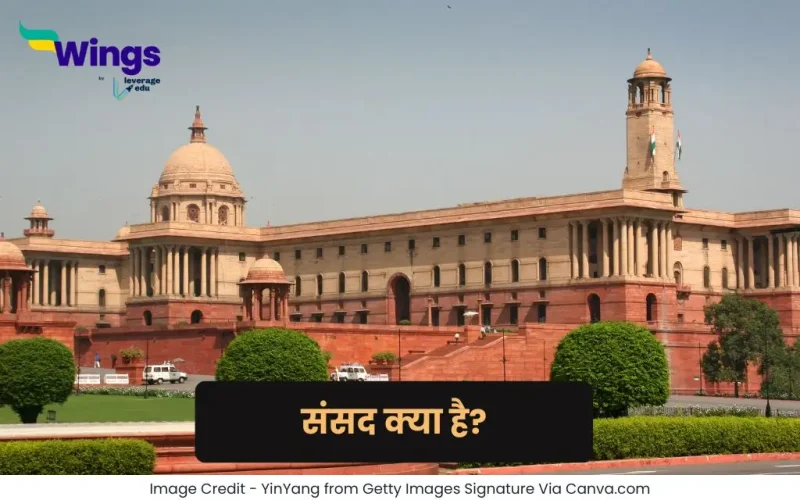

 45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!
45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!