बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास बुनियादी जीवन के आधार पर हुआ था। यह शिक्षा एक छात्र के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर आधारित है।
मध्यकाल में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों के आधार पर विचारधारा एक पूर्ण शिक्षा प्रणाली में बदल गई है, जिसे हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने तर्क दिया कि परम ज्ञान या ‘अनुत्तर-सम्यक-संबोधि’ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि यह पहले से उपस्थित है और व्यक्ति को इसका पता लगाने के लिए स्वयं के दायरे में जाने की जरूरत है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली भगवान बुद्ध के कुछ प्रमुख उपदेशों पर ही आधारित है। इस ब्लॉग में बौद्ध शिक्षा प्रणाली, इसके उद्देश्य, विशेषताएं आदि के बारे में विस्तार से दिया गया है।
This Blog Includes:
- बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या है?
- बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे?
- बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं जानिए
- बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम
- प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का इतिहास
- बौद्ध शिक्षा की विधियां क्या हैं?
- बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र कितने हैं?
- बौद्ध शिक्षा के लिए बेस्ट बुक्स के नाम
- बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान जानिए
- FAQs
बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या है?
बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास बुनियादी जीवन के आधार पर हुआ था। यह शिक्षा एक छात्र के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर आधारित है। यह छात्रों को संघ के नियमों का पालन करने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बौद्ध शिक्षा मूल रूप से भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई थी और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह सभी जातियों के लिए मठवासी और समावेशी थी जबकि उस समय भारत में जाति व्यवस्था, व्यापक रूप से प्रचलित थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समग्र विकास को सुगम बनाना है, चाहे वह बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी हो।
बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे?
बौद्ध शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जो इस प्रकार हैं:
- चरित्र का निर्माण करना- चरित्र निर्माण के लिए जरूरी नियमों का निर्धारण किया गया था, जिसमें आत्म-संयम, करूणा और दया पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था।
- व्यक्तित्व का विकास करना- आत्म संमय, आत्म निरर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, करूणा तथा विवेक जैसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणों का विकास कर छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्ध कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
- सर्वांगीण विकास- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्र के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को ध्यान मे रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी, साथ ही उसके व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखकर किसी कला-कौशल व उद्योग की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस तरह व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के समान विकास पर ध्यान दिया जाता था।
- बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करना- बौद्ध दर्शन में धर्म को संस्कृति का अंग माना गया है तथा संस्कृति के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण हो सकता है। इसके अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना शामिल था।
- मोक्ष की प्राप्ति- बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार के सभी दुःखों का एक मात्र कारण अज्ञानता है। अतः बौद्ध कालीन शिक्षा मे छात्रों को सच्चे एवं सार्थक ज्ञान के विकास पर बल दिया जाता था। बौद्ध काल मे सच्चे ज्ञान से अभिप्राय धर्म एवं दर्शन के चार सत्यों के ज्ञान और उसी के अनुरूप आचरण करने से था, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सके।
बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं जानिए
बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई है-
- शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी।
- शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार (initiation rites) होता था।
- शिक्षा समाप्ति पर उप- सम्पदा संस्कार होता था।
- अध्ययन काल 20 वर्ष का होता था जिसमें से 8 वर्ष प्रवज्या व 12 वर्ष उप- सम्पदा का समय होता था।
- पाठ्य विषय संस्कृत, व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि प्रमुख थे। इनके साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी साथ ही धनुर्विद्या एवं अन्य कुछ कौशलों की शिक्षा भी दी जाती थी।
- रटने की विधि पर बल दिया जाता था। इसके साथ वाद- विवाद, व्याख्यान, विश्लेषण आदि विधियों का प्रयोग भी किया जाता था।
- व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत भवन निर्माण, कढ़ाई- बुनाई, मूर्तिकला व अन्य कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। मुख्यतः कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी।
- छात्र जीवन वैदिक काल से भी कठिन था व गुरु – शिष्य में पिता-पुत्र समान घने सम्बन्ध थे।
- लोकभाषाओं में भी शिक्षा दी जाती थी।
- शिक्षा को जनतंत्रीय आधार दिया गया।
बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम
बौद्ध कालीन शिक्षा आध्यात्मिक सार थी। इसका मुख्य आदर्श निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति था। बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों से ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। अध्ययन का मुख्य विषय विनय और धर्म था। बौद्धिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया-
प्राथमिक शिक्षा
प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की थी। इन 6 वर्षों के प्रथम 6 माह छात्रों को सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी जिसकी सहायता से बच्चों को पाली भाषा के 49 वर्ण सिखाए जाते थे। 6 माह के बाद छात्रों को शब्द विद्या (आकृति विज्ञान), शिल्प कला विद्या, चिकित्सा विद्या (आयुर्वेद), तर्क विद्या एवं अध्यात्म विद्या के साथ साथ बौद्ध धर्म के सामान्य सिद्धांत भी बताये जाते थे।
उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा की समय अवधि लगभग 12 वर्ष थी। इनमें छात्रों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं दर्शन का ज्ञान दिया जाता था। व्याकरण एवं साहित्य के साथ पाली, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान भी दिया जाता था। इस पाठ्यक्रम में खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड शास्त्र के विषय भी शामिल थे।
भिक्षु शिक्षा
उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद जो विद्यार्थी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता था उससे भिक्षु शिक्षा संपन्न करनी होती थी। भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की होती थी। इसके अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ज्ञान दिया जाता था। भिक्षु शिक्षा में पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला धार्मिक और दुसरा लौकिक।
धार्मिक पाठयक्रम
इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था जिसके लिए तीन बौद्ध साहित्य पढ़ाए जाते थे- सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन्हें विस्तृत रूप में त्रिपिटक कहा जाता है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना और मोक्ष प्राप्त करना था।
लौकिक पाठ्यक्रम
इसके अंतर्गत गणित, कला, कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। जिससे छात्रों को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके।
प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का इतिहास
भारत में महत्मा बुद्ध के समय में समाज में जातिगत भेदभाव था। यह भेदभाव मनुष्य के पेशे के अनुसार और जन्म के अनुसार था। समाज में मनुष्य के चार विभाग थे जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ था। ब्राह्मणवाद समाज पर हावी हो गया और देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उन्हें धार्मिक प्रशिक्षण और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अन्य श्रेणी के लोग अपने धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित हैं। उस समय अस्तित्व में 62 विधर्मी सिद्धांत थे और पुरोहितवाद का बोलबाला था। इस पृष्ठभूमि में 600 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में एक धार्मिक क्रांति शुरू हुई और एक नया सिद्धांत या प्रणाली विकसित हुई जिसे बौद्ध सिद्धांत या बौद्ध दर्शन कहा जाता है।
बौद्ध धर्म की नींव पर प्राचीन भारत में एक नई और विशेष शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म ने एक व्यापक बदलाव लाया जिसने प्राचीन भारत या प्राचीन बौद्ध दुनिया में शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सर्वविदित है कि भारत में बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता के स्वर्ण युग का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव में भारतीय सभ्यता के सभी पहलुओं में प्रगति हुई। शिक्षा के कई केंद्र उभरे जो पहले मौजूद नहीं थे।
अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और देश भर में हजारों मठों का निर्माण हुआ। शिक्षा में सुधार करने और बौद्ध विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति, अनुदान और अन्य लाभ उपलब्ध कराए गए। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना और शिक्षकों को भूमि तथा पेंशन उपहार में देना इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में से कुछ थे।
बौद्ध शिक्षा की विधियां क्या हैं?
बौद्ध शिक्षा की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं:
- मौखिक विधि- वैदिक युग में सीखने का तरीका मुख्य रूप से मौखिक था। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते थे। एक विशेष पाठ को समझने वाले छात्र प्रचुर मात्रा में विषयों को रट कर सीखते थे।
- आगमनात्मक विधि- कई मठवासी स्कूलों और विहारों ने विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए तर्क या हेतु विद्या की आगमनात्मक पद्धति को शामिल किया। इस पद्धति के अनुसार ऐसे तथ्यों से अध्ययन प्रारंभ किया जाता है जो या तो ऐतिहासिक होते हैं या किसी प्रयोग द्वारा प्राप्त निर्णय के परिणाम होते हैं। इनमें छात्रों के बौद्धिक विकास लाने वाले तर्कों की चर्चा शामिल थी।
- निगरानी विधि- निगरानी विधियों की सहायता से, कई अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाने और अनुशासित करने की जिम्मेदारी भी प्रदान की जाती थी।
- परियोजना विधि- सैद्धांतिक और व्यावहारिक परियोजना प्रदान किए जाते थे, जिससे छात्र के कौशल का आंकलन किया जाता था।
बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र कितने हैं?
बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए देशभर में कई मठ एवं विहारों का निर्माण हुआ जहां बौद्धिक शिक्षा प्रदान की गई। बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र नीचे दिए गए हैं-
- तक्षशिला
- नालंदा
- विक्रमशिला
- वल्लभी
- मिथिला
- उदंतपुरी
- सारनाथ
- नदिया
- जगदला
- कांची
बौद्ध शिक्षा के लिए बेस्ट बुक्स के नाम
यहां कुछ बेहतरीन पुस्तकें हैं जो आपको बौद्ध शिक्षा प्रणाली का सार समझा सकती हैं-
| पुस्तक | लिंक |
| Buddhist Logic and Epistemology by Bimal Krishna Matilal | Buy Here |
| Buddhist System of Education Modern Approach by V. Nithiyanandam | Buy Here |
| Ancient Indian Education: Brahmanical and Buddhist by Radha Kumad Mookerji | Buy Here |
| Buddhist System of Education by Y Nithiyanandam | Buy Here |
| Buddhist Psychology: The Foundation of Buddhist Thought by Geshe Tashi Tsering, Lama Thubten Zopa Rinpoche | Buy Here |
बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान जानिए
आधुनिक भारतीय शिक्षा पर बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रभाव निम्न प्रकार दिखाई देता है-
- सभी धर्मों, वर्गों, व जातियों के बालकों के लिए शिक्षा में समान अक्सर उपलब्ध कराना- महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध मठ एवं विहार, प्रत्येक जाति, वर्ण तथा धर्म के बालकों को शिक्षा में समान अवसर के लिए समान रूप से खोलें। आज वर्तमान समय में भी बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त है। यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन है।
- विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण- बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया गया। और साथ ही बौद्ध मठों एवं विहारों में पुस्तकालय भी थे। वर्तमान समय में भी विद्यालयों में ही पुस्तकालय उपलब्ध होते है।
- गुरु और शिष्य के बीच मधुर सम्बन्ध- बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत गुरु और शिष्य के बीच मधुर सम्बन्ध थे। बौद्ध काल की तरह आज भी और अध्यापक के मध्य सम्बन्धों में आदर का भाव निहित होता है।
- नैतिक शिक्षा- बौद्ध काल में छात्रों को चारित्रिक विकास करने के लिए, उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है थी जो आज भी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनी हुई हैं।
- अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास करना- बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में प्रवेश के लिए आचरण सम्बन्धी नियमों का पालन करने की शपथ लेनी पड़ती थी जिससे छात्रों में अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास होता था। वर्तमान में भी शिक्षा के द्वारा छात्रों के अंदर अनुशासन लाने की व्यवस्था बरकरार है।
FAQs
आत्म संमय, आत्म निरर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, करूणा तथा विवेक जैसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणों का विकास कर छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्ध कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध मठ एवं विहार, प्रत्येक जाति, वर्ण तथा धर्म के बालकों को शिक्षा में समान अवसर के लिए समान रूप से खोलें। आज वर्तमान समय में भी बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त है। यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन है।
पाठ्य विषय संस्कृत, व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि प्रमुख थे। इनके साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी साथ ही धनुर्विद्या एवं अन्य कुछ कौशलों की शिक्षा भी दी जाती थी। रटने की विधि पर बल दिया जाता था। इसके साथ वाद- विवाद, व्याख्यान, विश्लेषण आदि विधियों का प्रयोग भी किया जाता था।
बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए देशभर में कई मठ एवं विहारों का निर्माण हुआ जहां बौद्धिक शिक्षा प्रदान की गई। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, उदंतपुरी आदि बौद्ध शिक्षा के कुछ प्रमुख केन्द्र है।
आशा है, आपको बौद्ध शिक्षा प्रणाली की सारी जानकारी मिली होगी। यदि आपको यह ब्लॉग पसंद आया है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य रोचक, ज्ञानवर्धक और आकर्षक ब्लॉग पढ़ने के लिए Leverage Edu Hindi Blogs के साथ बने रहें।
-
Highly excellent article .Thnx sir

 One app for all your study abroad needs
One app for all your study abroad needs
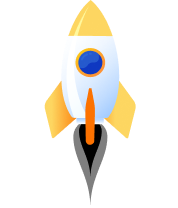


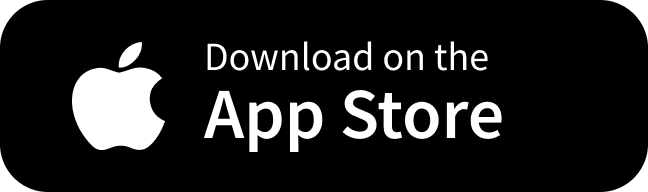











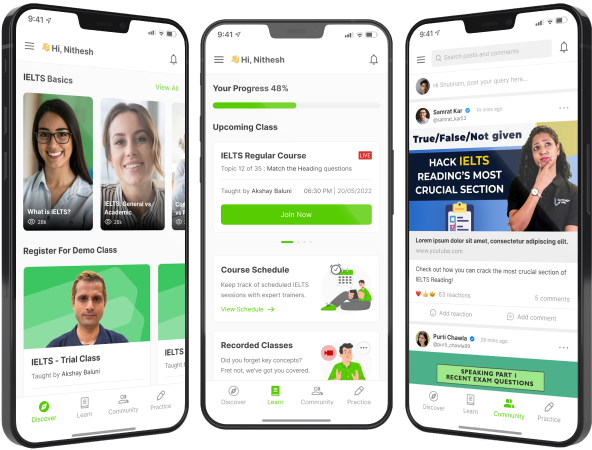



 45,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today.
45,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today.


1 comment
Highly excellent article .Thnx sir