गुप्त साम्राज्य (Gupta Dynasty in Hindi) के दो महत्वपूर्ण राजा हुए, समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ई तक शासन में रहा। 463-473 ई में सभी गुप्त वंश के राजा थे, केवल नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर। लादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे-धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमश : श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम (महेंद्रादित्य) और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केन्द्रीय शक्ति नहीं थी , जो अलग-अलग छोटे-बड़े राज्यों को विजित कर एकछत्र शासन-व्यवस्था की स्थापना कर पाती । यह जो काल था वह किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था । फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानायकों का विनाश हो रहा था ।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी
Table of contents
- गुप्त राजवंश का प्रारम्भिक इतिहास (Early History of Gupta dynasty in Hindi)
- गुप्त राजवंश के इतिहास के साधन ( (Tools of History of Guptas Dynasty) )
- Gupta Dynasty in Hindi: स्मारक
- Gupta Dynasty in Hindi: उत्पत्ति और उनका निवास स्थान
- गुप्त राजवंश के मूल निवास-स्थान (Original Habitat Places of Gupta Dynasty)
- गुप्त वंश की राजधानी क्या थी?
- Gupta Dynasty in Hindi: गुप्ता वंश के शासक (गुप्त वंश)
गुप्त राजवंश का प्रारम्भिक इतिहास (Early History of Gupta dynasty in Hindi)
Gupta dynasty in Hindi के इस लेख में गुप्त राजवंश की स्थापना ईस्वी 275 में महाराजा गुप्त द्वारा कराई गई थी । हमें यह निश्चित रूप से अभी तक पता नहीं है कि उसका नाम श्रीगुप्त था या केवल गुप्त था । उस विषय पर कोई भी लेख अथवा सिक्का अभी तक नहीं मिला ।दो मुहरें है जिनमें से
- एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृत मिश्रित मुद्रालेख ‘गुप्तस्य’ अंकित किया गया है
- दूसरे के ऊपर संस्कृत में ‘श्रीगुप्तस्य’ अंकित किया गया है।
यह पता चलता है कि गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ था,जो श्रीगुप्त का पुत्र था । यह जानने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्रों में केवल उसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक (आदिराज) बताया गया है । स्कन्दगुप्त के सुपिया (रीवा) के सभी लेख में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के बारे में पहले के समय से ही प्रारम्भ होती है । इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह भी सुझाव है कि वस्तुतः घटोत्कच ही इस वंश का संस्थापक था। गुप्त या श्रीगुप्त में से कोई भी आदि पूर्वज रहा होगा जिसके नाम का आविष्कार गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिये कर लिया गया होगा ।
परंतु इस प्रकार का किसी भी प्रकार का निष्कर्ष तर्कसंगत करना नहीं है , गुप्त लेखों के विषय में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है , यह जानने को मिलता है कि ऐसा इस बात का प्रतीत होता है कि यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी परंतु शायद उसके समय में यह वंश महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था । यह लगता है कि घटोत्कच के काल में ही सबसे पहले गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनैतिक महत्व प्राप्त की होगी ।
यह पता लगता है कि अल्तेकर और आर. जी. बसाक का विचार है कि उसी समय के काल में गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के बारे में स्थापित शायद किया गया होगा । इसी कारण कुछ अनेक प्रकार के लेखों में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का राजा कहा गया है । उसके भी संबंधित कोई लेख अथवा सिक्के अभी तक नहीं मिलते । इन दोनों शासकों की किसी भी प्रकार की उपलब्धि के विषय के बारे में हमें पता नहीं है । यह लगता है कि इन दोनों के नाम के पूर्व ‘महाराज’ की उपाधि को देखकर लगता है कि अधिकांश विद्वानों ने उनकी स्वतंत्र स्थिति में संदेह व्यक्त किया होगा और उन्हें सामन्त शासक बताया है । काशी प्रसाद जायसवाल का यह विचार है कि गुप्तों के पूर्व मगध पर लिच्छवियों का शासन हुआ करता था तथा साथ ही प्रारंभिक गुप्त नरेश उन्हीं के सामन्त हुआ करते थे ।
सुधाकर चट्टोपाध्याय के मतानुसार मगध पर तीसरी शती में मुरुण्डों का शासन हुआ करता था और साथ ही महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत हुआ करते थे । फ्लीट और बनर्जी की धारणा यहां भी है कि वे शकों के सामंत थे जो तृतीय शताब्दी में मगध के शासक हुआ करते थे । सबसे पहले चन्द्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को शकों की अधीनता से मुक्त करवाया था । परंतु इस प्रकार ऐसी विविध मतमतान्तरों के बीच यह निश्चित रूप से बताना कठिन हो सकता है कि प्रारम्भिक गुप्त नरेश किस सार्वभौम शक्ति की अधीनता स्वीकार किया करते थे ।
Check It: 10 डिप्लोमा कोर्स लिस्ट
पुनश्च यह भी निश्चित नहीं बता सकते कि वे सामन्त रहे हो । प्राचीन भारत में ऐसे कई सारे स्वतंत्र राजवंशों थे,
जैसे-
- लिच्छवि,
- मघ,
- भारशिव,
- वाकाटक आदि
यह सभी राजवंशों के शासक केवल ‘महाराज’ की उपाधि ही ग्रहण करते थे । ‘महाराजाधिराज’ की उपाधि का प्रयोग सबसे पहले चन्द्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। ऐसा इस बात का प्रतीत होता है कि शकों में प्रयुक्त क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुकरण करने पर ही उन्होंने ऐसा शायद शायद किया होगा । फिर बाद के भारतीय शासकों ने इस परंपरा का अनुकरण किया था और ‘महाराज’ की उपाधि सामन्त-स्थिति की सूचक बनाई गयी थी । वास्तविकता जो भी हो, इतना स्पष्ट होता है कि महाराज गुप्त और घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक हुआ करते थे जिनका राज्य संभवतः मगध के आस-पास ही सीमित था । इन दोनों महान राजाओं ने 319-20 ईसवी के लगभग आसपास राज्य किया था ।
गुप्त राजवंश के इतिहास के साधन ((Tools of History of Guptas Dynasty))

गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक और पुरातत्वीय दोनों ही प्रमाणों से हमें ज्ञात कराता है । साहित्यिक साधनों में पुराण सबसे ऊपर हैं । पुराणों में
- विष्णु,
- वायु
- ब्रह्माण्ड
तीनों को पुराणों में हम गुप्त-इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं ।
इनसे हमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है । विशाखदत्त कृत ‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ नाटक से गुप्तवंशी नरेश रामगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ बारे में सूचना मिलती है । उस समय अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते हैं । उनकी ऐसे अनेकानेक रचनाओं से गुप्तयुगीन समाज साथ ही संस्कृति पर सुन्दर तरह का प्रकाश पड़ता है । शूद्रककृत ‘मृच्छकटिक’ और वात्स्यायन के ‘कामसूत्र’ से भी गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था साथ ही नगर जीवन के विषय में रोचक के बारे में सामग्री मिल जाती है । भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के बारे में विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मैं हुआ है । ऐसे प्रकार के यात्रियों में फाहियान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय किया गया है , वह एक चीनी यात्री था । फाहियान गुप्तनरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (375-415 ईस्वी) के शासन काल के समय में भारत आया था।

उसने ही मध्यदेश की प्रजा का वर्णन किया है । सातवीं शती के चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय के बारे में हमें सूचनायें मिलती हैं । यह पता चलता है कि उसने कुमारगुप्त प्रथम (शक्रादित्य), बुध गुप्त, बालादित्य आदि बहुत सारे गुप्त शासकों का उल्लेख किया है , साथ ही इसके बारे में विवरण से हमें यह पता चलता कि कुमारगुप्त ने ही उस समय नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी । वह ‘बालादित्य’ को हूण नरेश मिहिरकुल का विजेता बताता है , उसकी पहचान नरसिंह गुप्त बालादित्य से करवाई जाती है । साहित्यिक साक्ष्यों के पुरातत्वीय प्रमाणों से भी हमें गुप्त राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पर्याप्त सहायता मिलती है ।
Samrat Ashoka History in Hindi
इनका वर्गीकरण तीन भागों में किया जा सकता है:
- अभिलेख,
- सिक्के
- स्मारक
इनका विवरण इस प्रकार है:
Abhilekh (अभिलेख)
गुप्तकालीन अभिलेखों में सबसे पहले उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भलेख के बारे में किया जा सकता है । यह एक प्रशस्ति है ,जिससे समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय यह सब उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि से मीला गुहालेख से उसकी दिग्विजय की के बारे में सूचना प्राप्त होती है । उस समय कुमारगुप्त प्रथम के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं जो इस बात का सूचक कराते है कि इस समय तक सम्पूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकार में आ गया था । स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ-लेख से हूण आक्रमण के बारे में यह सूचना मिलती है । Gupta dynasty in Hindi में इसी सम्राट के जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से हमें इसके बारे में यह पता चलता है कि उसने इतिहास-प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था ।

इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के अभिलेख एवं दानपत्र मिले हैं जिनसे हमें यह पता चलता है की गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है । इन सभी अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत मैं दी गई है तथा इनमें दी गयी तिथियाँ ‘गुप्त संवत्’ की हैं । इतिहास के साथ साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त अभिलेखों का विशेष महत्व होता है । इसे संस्कृत भाषा और साहित्य के पर्याप्त विकसित होने के बारे में प्रमाण मिलता है । हरिषेण द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्ति तो वस्तुतः एक प्रकार का क्षचरित-काव्य ही है ।
सिक्के (Sikke)

Gupta dynasty in Hindi के इस ब्लॉग में हमें गुप्तवंशी राजाओं के अनेक प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं ।
- स्वर्ण,
- रजत
- तांबे
स्वर्ण सिक्कों को ‘दीनार कहा जाता था’, रजत सिक्कों को ‘रुपक’ या रुप्यक कहा जाता था ,तथा ताम्र सिक्कों को ‘माषक’ कहा जाता था । गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें राजस्थान प्रान्त के बयाना से प्राप्त हुआ है ।
इससे इस बारे में स्पष्ट होता है कि चन्द्रगुप्त ने लिच्छवि राजकन्या कुमारदेवी के साथ विवाह किया था । समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से उसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना हुई थी तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र-हनन प्रकार के सिक्कों से उसकी पश्चिमी भारत (शक-प्रदेश) के विजय के बारे में सूचना मिलती है ।
मध्य प्रदेश के एरण और भिलसा से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि उसकी ऐतिहासिकता का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त करते हैं । कभी-कभी सिक्कों के अध्ययन से हमें उनके काल के बारे में राजनैतिक तथा आर्थिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त भी होता है । जैसे कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्कों से पतनोन्मुख आर्थिक दशा के बारे मेंआभास मिलता है । इनमें मिलावट की मात्रा अधिक होता है ।
Gupta Dynasty in Hindi: स्मारक

गुप्तकाल के अनेक प्रकार के मन्दिर, स्तम्भ मूर्तियों और चैत्य-गृह (गुहा-मन्दिर) का प्राप्त होते हैं जिनसे तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की उत्कृष्टता के बारे में सूचित होती है । इनसे तत्कालीन सम्राटों एवं जनता के धार्मिक विश्वास को समझने में के लिए मदद भी मिलती है ।
मन्दिरों के बारे में विशेष उल्लेखनीय है
- भूमरा का शिव मन्दिर,
- तिगवाँ (जबलपुर) का विष्णु मन्दिर,
- नचना-कुठार (मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अजयगढ़ रियासत में वर्तमान) का पार्वती मन्दिर,
- देवगढ़ (झांसी) का दशावतार मन्दिर,
- भितरगाँव (कानपुर) का मन्दिर
- लाड़खान (ऐहोल के समीप)
ये सभी मन्दिर अपनी निर्माण-शैली, आकार-प्रकार एवं सुदृढ़ता के लिये प्रसिद्ध हुआ करते थे हैं और वास्तुकला के भव्य नमूने हैं । मन्दिरों के अतिरिक्त
- सारनाथ,
- मथुरा,
- सुल्तानगंज,
- करमदण्डा,
- खोह
- , देवगढ़
स्थानों से बुद्ध, शिव, विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं ।
मन्दिर तथा मूर्तियों के साथ ही साथ
- बाघ (ग्वालियर, म. प्र.)
- अजन्ता की कुछ गुफाओं (16वीं एवं 17वीं) के चित्र भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं ।
बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से सम्बन्धित है और अजन्ता के चित्रों का विषय धार्मिक से संबंधित है । इन चित्रों के माध्यम से गुप्तकालीन समाज की वेष-भूषा, श्रुंगार-प्रसाधन और धार्मिक विश्वास को समझने के बारे में सहायता मिलती है । साथ ही इनसे गुप्तयुगीन चित्रकला के पर्याप्त विकसित होने का भी प्रमाण भी साथ में उपलब्ध हो जाता है ।
Check it: भारत में लाइब्रेरी साइंस कॉलेज [Library Science Colleges in India]
Gupta Dynasty in Hindi: उत्पत्ति और उनका निवास स्थान
Gupta dynasty in Hindi के इस ब्लॉग में यह जानने में आया है कि यद्यपि गुप्त नरेशों के अनेक अभिलेख तथा सिक्के मिले हैं, तथापि उनमें किसी से भी न तो उनके वर्ण अथवा जाति के विषय में कोई संकेत मिलता है, न ही साहित्यिक साक्ष्यों से कोई ठोस सामग्री उपलब्ध होती है । फलस्वरूप गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीन समय के भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है । विद्वानों ने इस राजवंश को शूद्र से लेकर ब्राह्मण जाति तक का सिद्ध करने का अलग-अलग प्रकार से प्रयास किया है ।
1. शूद्र अथवा निम्न उत्पत्ति का मत:
Gupta dynasty in Hindi के इस ब्लॉग में गुप्तों को शूद्र अथवा निम्न जाति से सम्बन्धित करने वाले विद्वानों में काशी प्रसाद जायसवाल का नाम सर्वाधिक बहुत ही महत्वपूर्ण है । जायसवाल की यह धारणा है कि गुप्त नरेशों ने निम्न वर्ण से सम्बद्ध होने के कारण ही अपने अभिलेखों में अपनी जाति के बारे में का उल्लेख नहीं किया है ।
अपने मत की पुष्टि के लिये उन्होंने ‘कौमुदी महोत्सव’ नामक एक नाटक ग्रन्थ का सहारा भी लिया है जिसकी रचना संभवतः वज्जिका नाम की किसी महान कवियित्री द्वारा किया था । इस नाटक में हमें यह एक कथा मिलती है जिसका सारांश इस प्रकार है- “मगध में सुन्दरवर्मा नामक एक क्षत्रिय राजा शासन किया करता था । परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था, उसने चण्डसेन नामक एक व्यक्ति को गोद लिया । चण्डसेन राजाओं में कारस्कर कहा गया है । कुछ समय के बाद सुन्दरवर्मा को कल्याणवर्मा नामक एक अपना पुत्र उत्पन्न हुआ था । कल्याणवर्मा के जन्म से चण्डसेन बड़ी निराशा पर्याप्त हुयी ।
उसने मगध के वैरी म्लेच्छ लिच्छवियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर एक नया अवसर पाकर कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) को अचानक से घेर लिया । फीर युद्ध में सुन्दरवर्मा मार डाला गया था और चण्डसेन मगध का राजा बन बैठा था । पाटलिपुत्र में कल्याणवर्मा के जीवन को असुरक्षित देखकर उसके पिता के योग्य तथा अनुभवी मन्त्रियों ने उसे ‘पम्पासर’ नामक स्थान में पहुँचा दिया ।
इसके बाद उन्होंने चण्डसेन के विरुद्ध विद्रोह भड़काया था। सीमान्त प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए जिन लोगों को दबाने के प्रयास में चण्डसेन अपने बन्धुओं सहित भार डाला गया था । उसकी मृत्यु के साथ ही साथ उसका वंश समाप्त हो चुका था । फिर तत्पश्चात् कल्याण वर्मा मगध का राजा हुआ ।”
जायसवाल महोदय ने इस ‘धारण’ गोत्र का समीकरण जाटों की धरणि शाखा के साथ किया है । इससे भी यही पता चलता है कि गुप्तवंशी नरेश उच्च वर्ण के नहीं थे । इसी सन्दर्भ में उन्होंने मत्स्यपुराण का यह भी कहा है कि ( कथन ) भी उद्धत किया है जिसमें ‘महानन्दी के बाद शूद्रयोनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे ।’ इस कथन से भी गुप्तों की निम्न के बारे में उत्पत्ति संकेतित होती है । इन सभी प्रमाणों के आधार पर जायसवाल महोदय गुप्तों को और शूद्रनिम्नजातीय प्रमाणित करने की चेष्टा के बारे में करते हैं ।
काशी प्रसाद जायसवाल के उपर्युक्त तर्क यद्यपि देखने में सबल प्रतीत होते हैं परन्तु यह भी पता चलता है कि यदि सावधानीपूर्वक उनकी समीक्षा की जाये तो ऐसा प्रतीत होगा कि उनमें कोई विशेष बल नहीं है । कौमुदीमहोत्सव नाटक में जिस चण्डसेन का उल्लेख हुआ है, उसकी यह भी पहचान गुप्तवंशी चन्दगुप्त प्रथम के साथ नहीं की जा सकती ।
नाटक के अनुसार यह पता चलता है कि युद्ध में चण्डसेन अपने बन्धु-बान्धवों के साथ मार डाला गया था। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही उसका वंश भी समाप्त हो गया । चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ ऐसी कोई भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई । हमें यह निश्चित रूप से पता चलता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी शताब्दियों तक उसका वंश चलता रहा ।
यदि हम चण्डसेन तथा चन्द्रगुप्त दोनों को एक व्यक्ति हैं ऐसा मान लें तो ऐसी स्थिति में Gupta dynasty in Hindi हमें गुप्तों का इतिहास चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ ही समाप्त कर देना होगा क्योंकि जो सर्वथा अस्वाभाविक घटना होगी , यानी कि चण्डसेन गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त नहीं हो सकता ।इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जे. एस. नेगी की यह धारणा है कि कौमुदी महोत्सव में प्रयुक्त ‘निहत:’ शब्द से चण्डसेन का मारा जाना सूचित नहीं होता ।
रामायण से उदाहरण देते हुये उन्होंने इस बात का स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संस्कृत की ‘हन्’ धातु का प्रयोग कभी-कभी विपत्ति अथवा अपमान को सूचित करने के लिये भी किया जाता है ।यहाँ चण्डसेन के अपमानित होने अथवा क्षणिक हानि उठाने से तात्पर्य बताया है ।
यह बात जान ने को मिलती है ,किन्तु इस प्रकार के विचार से सहमत होना कठिन है क्योंकि नाटक में चण्डसेन के प्रसंग में यह भी कहा गया है कि उसका कुल उन्मूलित कर दिया गया । इस शब्द से उसके विनाश की सूचना मिलती है, न कि केवल अपमानित किये जाने की ।
अधिकांश विद्वान कौमुदी महोत्सव की ऐतिहासिकता में थोड़ा बहुत सन्देह करते हैं । क्षेत्रेश चन्द चट्टोपाध्याय ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में उल्लिखित ‘कृतिवासस्’ शब्द की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है । इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो शंकर से है परन्तु इसका लाक्षणिक अर्थ शंकराचार्य भी होता है क्योंकि इसमें ‘कृतिवासस् को द्वैत की गाँठ का भेदन करने वाला’ (नानात्व ग्रन्थि-भेत्री) के बारे में कहा गया है ।
इस बात से स्पष्ट होता है कि इससे तात्पर्य अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य से ही है जिनका समय 781-820 ईस्वी माना जाता है । इस ग्रन्थ में शंकराचार्य का उल्लेख होना यह सिद्ध करता है कि यह बहुत समय बाद की रचना है । यानी कि गुप्त-इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे सहायक नहीं माना जा सकता ।
इस प्रकार कहां जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव के आधार पर गुप्तों की जाति के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं लगता । जहां तक यह लगता है कि ‘चान्द्र व्याकरण’ का प्रश्न है, सभी विद्वान् इस मत के नहीं हैं कि इसमें गुप्तों के लिये ‘जर्ट’ शब्द का प्रयोग हुआ है । हर्नले ने जर्ट के स्थान पर ‘जप्त’ पाठ पढ़ा है ।
ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगोमिन् की मूल पाण्डुलिपि में ‘गुप्त’ पाठ ही रहा होगा जिसे कालान्तर में लिपि की भूल से जर्ट या जप्त के विषय में लिक दिया गया । इस बात से यह पता चलता है कि इसमें गुप्तों की जाति के विषय में अपमानजनक कुछ भी नहीं है । जहाँ तक पूना ताम्रपत्र के धारण गोत्र का प्रश्न है, इसकी पहचान जाटों की धरणि शाखा से नहीं की जा सकती क्योंकि इन दोनों शब्दों में उच्चारण के अतिरिक्त कोई दूसरी समानता नहीं दिखाई रही है ।
हम यह कह सकते हैं कि मत्स्यपुराण का कथन केवल नन्दों तक ही सीमित है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि महानन्दी के बाद शासन करने वाले सभी राजा शूद्र थे । जैसे-
- मौर्य क्षत्रिय थे,
- शुंग , सातवाहन ब्राह्मण थे ।
इस विवेचन के आधार पर हम इस बात को गुप्तों को शूद्र और निम्न जाति का नहीं मान सकते हैं ।
100 Motivational Quotes in Hindi
2. वैश्य होने का मत:
- एलन, एस. के. आयंगर,
- अनन्त सदाशिव अल्टेकर,
- रोमिला थापर,
- रामशरण शर्मा
उनके जैसे कुछ महान विद्वान् गुप्तों को वैश्य मानते थे । अपने मत के समर्थन में अल्टेकर महोदय ने विष्णुपुराण के एक श्लोक का सहारा लिया है जिनके अनुसार अपने अंत के शब्द में बदलाव किया
- ‘ब्राह्मण अपने नाम के अन्त में शर्मा शब्द,
- क्षत्रिय वर्मा शब्द,
- वैश्य गुप्त शब्द
- शूद्र दास शब्द लिखेंगे ।’
उन्होंने जब गुप्त राजाओं के नामान्त में ‘गुप्त’ शब्द जुड़ा देखकर तो अल्टेकर उन्हें वैश्य जाति से सम्बन्धित करते हैं । उनके मतानुसार यह देखा गया कि गुप्त युग तक आते-आते वर्णों के अनुसार व्यवसाय-चयन का सिद्धान्त शिथिल पड़ गया था । वह सभी लोग ब्राह्मण क्षत्रियों का काम करने लगे थे, जैसे वाकाटक और कदम्ब वंशों के लोग ब्राह्मण होते हुये भी शासन का कार्य करते थे । Gupta dynasty in Hindi में गुप्तकालीन रचना शूद्रकृत ‘मृच्छकटिक’ में चारूदत्त नामक एक ब्राह्मण को ‘सार्थवाह’ (व्यापारी) के रूप में कहा गया है । यह कह सकते हैं कि गुप्त लोग यदि वैश्य होते हुये भी शासन करते थे तो इस विषय में हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये । यह देखा गया कि अल्टेकर का उपर्युक्त मत कई दृष्टियों से विचारणीय है । सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि Gupta dynasty in Hindi के दूसरे सम्राट घटोत्कच के नाम के अन्त में ‘गुप्त’ शब्द नहीं जुड़ा मिलता है । अभिलेखों में उसे केवल महाराजा घटोत्कच ही के नाम से कहा गया है । वास्तविकता यह है कि ‘गुप्त’ नाम इस वंश के संस्थापक का था और सबसे पहले चन्द्रगुप्त प्रथम ने इसे अपने नाम के अन्त में प्रयुक्त किया था ।
यह देखने को मिला कि कालान्तर में सभी राजाओं ने इसका अनुकरण किया । यह भी कहा गया कि पुनश्च ‘गुप्त’ शब्द धारण करना केवल वैश्य वर्ण के लोगों का ही एकाधिकार नहीं था । प्राचीन समय भारतीय साहित्य से हमें अनेक नाम ऐसे मिलते हैं जो यद्यपि वैश्य नहीं थे और उन्होंने गुप्त शब्द का अपने नामान्त में धारण किया था । उदाहरण के लिये देख सकते हैं कि कौटिल्य, जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था, का एक नाम विष्णुगुप्त भी था । इसी प्रकार कुछ अन्य नाम भी प्राचीन साहित्य काल और लेखों से खोजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं। इस बात का भी संकेत होता है कि केवल गुप्त शब्द के ही आधार पर गुप्त राजवंश को वैश्य वर्णान्तर्गत रखना समीचीन नहीं होगा ।
3. क्षत्रिय होने का मत:
- सुधाकर चट्टोपाध्याय,
- रमेशचन्द्र मजूमदार,
- गौरीशंकर हीराचन्द ओझा आदि
ऐसे कुछ महान विद्वान्, गुप्तों को क्षत्रिय जाति से बारे में सम्बन्धित करते हैं ।
इनके सभी तर्कों का सारांश इस कुछ इस प्रकार है:
- पंचोभ (बिहार के दरभंगा जिले में स्थित) से प्राप्त एक लेख में किसी गुप्तवंश के बारे में उल्लेख हुआ है ।
- जावा से प्राप्त ‘तन्त्रीकामन्दक’ नामक ग्रन्थ में महाराजा ऐश्वर्यपाल के बारे में उल्लेख मिलता है ।
- सिरपुर के लेख में चन्द्रगुप्त नामक राजा को चन्द्रवंशी क्षत्रिय के बारे में कहा गया है ।
- गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध था इसलिए लिच्छवियों को क्षत्रिय के नाम से माना गया है।
परन्तु ये सभी कुछ तर्क तक निर्बल हैं ।
इनकी समीक्षा हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं:
- पंचोभ के लेख में जिस गुप्त वंश का के बारे में उल्लेख हुआ है वह गुप्त राजवंश नहीं प्रतीत होता।
- यह भी देखा गया कि तन्त्रीकामन्दक एक मध्यकालीन रचना है जिसे गुप्त-इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक नहीं मात्रा जा सकता ।
- यह भी देखने में आया कि सिरपुर अभिलेख का चन्द्रगुप्त गुप्तवंशी नहीं प्रतीत होता क्योंकि दोनों की वंश परम्परायें अलग-अलग हैं ।
- यह का सत्य है कि सभी विद्वान् इस मत के नहीं है कि लिच्छवि क्षत्रिय थे । पालि ग्रन्थों में उन्हें ‘खत्तिय’ कहा गया है जो राजसत्ता के बारे में सूचक है । यह भी देखने में आया है कि मनु ने उन्हें ‘व्रात्य’ (धर्मच्युत) कहा है जो सावित्री के अधिकार से वंचित एवं संस्कारों से विहीन होते थे ।
Gupta dynasty in Hindi के इस ब्लॉग में यह कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी राजनैतिक प्रभुता के कारण ही उन्हें ‘क्षत्रिय’ स्वीकार कर लिया गया था । उस समय में पुनश्च यदि लिच्छवि क्षत्रिय रहे भी ही तो भी हम गुप्ता को उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध आधार पर क्षत्रिय नहीं मान सकते क्योंकि प्राचीन भारत में अनुलोम विवाह शास्त्र संगत था जिसके अनुसार कन्या अपने से ऊपर वर्ण में ब्याही जाती थी । इस बारे में यह कह सकता है कि इन तर्कों के आलोक में गुप्तों को क्षत्रिय मानने का मत ज्यादा सबल नहीं प्रतीत होता ।
4. ब्राह्मण होने का मत:
उस समय देखा गया था कि गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिये गये हैं उनमें उनको ब्राह्मण जाति से सम्बन्धित के साथ करने का मत कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता है । यहाँ इस बात का उल्लेखनीय है कि गुप्तवंशी लोग ‘धारण’ गोत्र के थे । इसके बारे में उल्लेख चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र के अंदर किया है। यह भी देखा गया था कि यह गोत्र उसके पिता का ही था क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय ‘विष्णुवृद्धि’ गोत्र का ब्राह्मण था, यह गोत्र ब्राह्मणों का था । हेमचन्द्र रायचौधरी ‘धारण’ का तादात्म्य शुंग शासक अग्निमित्र की प्रधान महिषी धारिणी, जिसका उल्लेख कालिदास के मालविकाग्निमित्र के अंदर मिलता है, उसे स्थापित करते हुये इस बात का प्रतिपादन करते है कि गुप्त लोग उसी के वंशज थे । यह देखने में आया है कि किन्तु इस प्रकार के निष्कर्ष के लिये कोई प्रमाण नहीं है । स्कन्दपुराण में ब्राह्मणों के चौबीस गोत्र गिनाये गये हैं ,जिनमें बारहवाँ गोत्र ‘धारण’ है । यह कह सकते हैं कि है कि दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्वान् यह मत रखते हैं कि प्राचीन भारत में लोग अपने पुरोहित का गोत्र भी धारण कर लेते थे । इस बात का संभव है प्रभावती गुप्ता का ‘धारणगोत्र’ उसके पिता का न होकर किसी पुरोहित का हो । साथ में यह देखा गया है कि किन्तु जैसा कि मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने स्पष्ट किया है, केवल क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लोग ही अपने पुरोहित का गोत्र धारण करते थे, न कि ब्राह्मण । प्रभावती गुप्ता चूँकि ब्राह्मण वर्ण की थी, इस बात का संभव है कि उसके द्वारा अपने पुरोहित के गोत्र को धारण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह देखा गया है कि कदम्ब वंश राजा काकुत्सवर्मा के तालगुण्ड (मैसूर) अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्तकुल (गुप्तादिपार्त्थिवकुलानि) में किया था । साथ में यह जानने को मिलता है कि कदम्बवंशी लोग मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण थे तथा उन्होंने अपने को हारीत का वंशज बताया है । इस वंश के संस्थापक मयूरशर्मा को कौटिल्य की प्रकृति का रूढ़िवादी ब्राह्मण के नाम से कहा गया है ।
यह कह सकता है कि कदम्ब नरेश ‘धर्ममहाराज’ एवं ‘धर्ममहाराजाधिराज’ की उपाधियाँ धारण करते थे । इस कुल के समय में कोई भी कन्याओं का विवाह वाकाटक तथा गंग जैसे ब्राह्मण कुलों में सम्पन्न हुआ था । इस बात का संदेह किया जा सकता है कि गुप्तों की शक्ति से डर कर अथवा उनकी समृद्धि से प्रभावित होकर कदम्बों ने शास्त्रोल्लंघन किया होगा । यह भी देखा गया है कि किन्तु हम यह जानते हैं कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी भी गुप्तवंशी शासक ने सुदूर दक्षिण में अभियान नहीं किया । तो हम कह सकते हैं कि कदम्बों द्वारा उनकी शक्ति से भयभीत होने का प्रश्न नहीं उठता । इस बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने समृद्धि के आगे धर्म का परित्याग किया होगा । उस समय पुनश्च गुप्तवंश की कन्याओं का विवाह भी ब्राह्मण में ही हुआ था । उस समय प्रभावतीगुप्ता वाकाटक कुल में ब्याही गयी थी । उस समय छठी शताब्दी के बौद्ध लेखक परमार्थ ने बताया कि बालादित्य ने अपनी बहन का विवाह वसुराट नामक ब्राह्मण से किया था । हम यह कह सकते हैं कि गुप्तों को ब्राह्मण मानना ही अधिक समीचीन लगता है । इस बात का ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अतिशय उदारता एवं धर्म-सहिष्णुता की नीति के कारण ही गुप्त राजाओं ने अपने अभिलेखों में अपने वर्ण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा है । इस प्रकार इन बहुत सारे मतों की समीक्षा करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि गुप्तों की जाति का प्रश्न हमारे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असंदिग्ध रूप से हल नहीं किया जा सकता । हमें इस बात को संभावित रूप से उन्हें क्षत्रिय अथवा ब्राह्माण वर्षों में किसी एक के साथ सम्बद्ध करना चाहिए , बहुत संभव है वे ब्राह्मण ही रहे हों ।
गुप्त राजवंश के मूल निवास-स्थान (Original Habitat Places of Gupta Dynasty)
1. बंगाल:
- एलन,
- गांगुली त्
- रमेश चन्द्र मजूमदार
जैसे कुछ महान विद्वान् गुप्तों का मूल निवास-स्थान बंगाल में निर्धारित करते हैं । यह कहा जाता है कि इस मत का मुख्य आधार चीनी यात्री इत्सिग का यात्रा विवरण है । यह देखने को मिला है कि यह लिखता है कि- ‘उसके 500 वर्षों पूर्व हुई-लुन नामक एक चीनी यात्री नालन्दा आया था । इसमें देखने को मिला है कि यहाँ चिलिकितो (श्रीगुप्त) नामक राजा ने चीनी भिक्षुओं के लिये मन्दिर बनवाया था तथा उसके निर्वाह के लिये चौबीस गाँवों की आमदनी दान में दिया था । यह ‘चिन का मन्दिर’ कहा जाता था और मि-लि-किया-सि-किया-पो-नो (मृगशिखावन) नामक मठ के पास स्थित था जिसकी दूरी नालन्दा से 40 योजन पूर्व की ओर गंगा नदी के किनारे पड़ती थी ।’ यह कहा जाता था कि इन विद्वानों ने श्रीगुप्त को गुप्तवंश का संस्थापक माना है । यह देखने को मिला जी गांगुली का विचार कि इत्सिग के आधार पर यदि नालन्दा से पूर्व की ओर गंगानदी के किनारे की 40 योजन (240 मील) वाली दूरी नापी जाये तो यह स्थान आधुनिक पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पड़ेगा । इसके बारे में उल्लेख किया गया कि यहीं गुप्तवंश के संस्थापक का मूल निवास था, मजूमदार के मतानुसार हमें इसे एक सम्भावित परिकल्पना के रूप में मान लेना चाहिए ।
परन्तु इस मत के विरुद्ध कुछ दो बातें कही जा सकती हैं कि:
- इस मत पर विरोध कुछ बातें यह है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम ‘महाराज गुप्त’ था जबकि चिलिकितो का भारतीय रूपान्तर श्रीगुप्त होता है ।
- इस मत पर विरोध कुछ बातें यह है कि चिलिकितो (श्रीगुप्त) का समय इत्सिग के अनुसार उसके 500 वर्षों पूर्व था ,इत्सिग 671 ईस्वी में भारत आया था ।
यह कहा जा सकता है कि उसने जिस शासक की चर्चा की है उसका समय 171 ईस्वी (671-500 ईस्वी) हुआ । यह देखने को मिला कि गुप्तवंश के संस्थापक का काल 275 ईस्वी के पूर्व नहीं हो सकता । साथ में यह भी कहा जा सकता है कि श्रीगुप्त तथा महाराज गुप्त दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं । उस समय इस प्रकार हम गुप्तों का आदि राज्य बंगाल में नहीं मान सकते । इस प्रसंग में एक अन्य विचारणीय बात यह देखने को मिलती है कि चिलिकितों द्वारा चौबीस गाँवों की आय दान में दिया जाना यह सिद्ध करता है कि चह एक शक्तिशाली तथा समृद्ध शासक था ।
उस समय किन्तु यह स्थिति श्रीगुप्त की स्थिति से मेल नहीं खाती जो पात्र एक साधारण तथा सम्भवत: अधीनस्थ राजा था । यह देखा गया था कि जे. एस. नेगी के अनुसार यह गुप्तवंश का कोई महान् सम्राट था । साथ में ऐसा लगता है कि चीनी यात्री ने राजा का व्यक्तिगत नाम नहीं दिया है, अपितु मात्र उसके वंश का उल्लेख किया है जिसका अर्थ है- ‘गुप्तवंश का प्रसिद्ध शासक ।’ यह कहा जा सकता है कि गुप्तों के मूल स्थान के निर्धारण में इत्सिग के विवरण को आधार नहीं बनाया जा सकता ।
2. मगध:
पुराणों पर दृष्टिपात करने से इस बात का ज्ञात होता है कि गुप्तों का आदि सम्बन्ध मगध से था । यह देखा गया था कि विन्टरनित्ज का विचार है कि विष्णुपुराण गुप्तकालीन रचना है, इस बात का संदेह होता है कि इसे गुप्तों के इतिहास के सम्बन्ध में प्रामाणिक माना जा सकता है । साथ में यह भी देखा गया था कि विष्णुपुराण की कुछ पांडुलिपियों में ‘अनुगंगा प्रयागं मागधा: गुप्ताश्च भोक्ष्यन्ति’ अर्थात् प्रयाग तथा गंगा के किनारे के प्रदेश पर मगध के गुप्त लोग शासन करेंगे, उल्लिखित मिलता है । यह कह सकते हैं कि ढाका से प्राप्त इस पुराण की तीन पाण्डुलिपियों में ‘अनुगंग प्रयागं च मागधा: गुप्ताश्च मागधान् भीक्ष्यन्ति’ उल्लेख है ।
दोनों पाठों का कुछ इस बातों का अन्तर इस प्रकार है:
- प्रथम पाठ में ‘अगुगंगा’ तथा द्वितीय पाठ में ‘अनुगंग’ मिलता है ।
- द्वितीय पाठ में गुप्ताश्च तथा भोक्ष्यन्ति के बीच ये ‘मागधान्’ शब्द निरर्थक जुड़ा हुआ है क्योंकि गुप्ताश्च का विशेषण मागधा: है । यह बता सकते है कि प्रथम पाठ अधिक शुद्ध लगता है ।यह देखने को मिलता है कि उपर्युक्त दोनों ही पाठों में ‘मागधा:’ शब्द ‘गुप्ताश्य’ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । हमें इस बात का इससे स्पष्ट है कि या तो मगध गुप्तों का मूल निवास था या यह उनके राज्य में सम्मिलित था । यह कहा जा सकता है कि वायुपुराण में किसी गुप्तशासक की साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ‘गंगा नदी के किनारे प्रयाग तथा साकेत और मगध के प्रदेशों का गुप्तवंश के लोग उपभोग करेंगे’ ।उस समय या देखने को मिला कि रायचौधरी का विचार है कि प्रयाग तथा कोशल (साकेत) के प्रदेश गुप्तवंश के तीसरे शासक महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा जीतकर गुप्त राज्य में मिलाये गये थे । यह भी देखा गया कि उत्तरी बिहार को चन्द्रगुप्त ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके प्राप्त किया था । इस बात को यह कह सकते हैं कि इस प्रकार ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तों का आदि राज्य मगध में ही था । इस बात का संदेह होता है कि मगध के साथ उनके मूल सम्बन्ध को ध्यान में रखकर ही पुराण उन्हें ‘मागध गुप्त’ कहते हैं ।
3. पूर्वी उत्तर-प्रदेश:
यह देखा गया था किएस. आर. गोयल ने गुप्तों की मूल भूमि का प्रश्न पुरातात्विक आधार पर हल करने का प्रयास किया है । यह कह सकते है कि उनके अनुसार किसी भी वंश के प्रारम्भिक लेख तथा सिक्के प्रायः उसी स्थान से प्राप्त होते हैं जो उसका आदि निवास होता है । उस समय यह देखा गया था कि बख्त्री-यवन शासकों के सिक्के बैक्ट्रिया से मिलते हैं । इस बात का संदेह होता है कि कनिष्क के अधिकांश लेख उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में तथा वाकाटकों के लेख भी उनके आदि स्थान से ही मिले हैं । साथ में यह भी कहा जा सकता है कि चूँकि गुप्तवंश के प्रारम्भिक लेख तथा सिक्के पूर्वी उत्तर-प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, इस बात से स्पष्ट होता है कि उनका मूल निवास स्थान इसी क्षेत्र में कहीं रहा होगा । यह लिखा गया था कि इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि गुप्तों के प्राचीनतम स्वर्ण सिक्के ‘चन्द्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार’ हैं । यह देखने को मिलता है कि इनमें से अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं । उस समय में प्रारम्भिक गुप्त लेखों में आठ इसी क्षेत्र से मिलते हैं । यह देखा गया था कि गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण लेख प्रयाग से मिला है जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का विवरण देता है । इस बात से यह संडे होता है कि इस प्रकार का लेख शासक की स्थान के प्रति अभिरुचि का सूचक है ।
उस समय या देखा गया था कि इस कोटि का दूसरा लेख यशोधर्मन् का मन्दसोर लेख है जो उसी स्थान से मिलता है जो उसकी शक्ति का केन्द्र था । इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुप्तों के जो लेख मिले हैं वे न केवल संख्या में अधिक हैं, अपितु वे अन्य स्थानों के लेखों से प्राचीनतर भी हैं। यार देखने को मिलता है कि इससे गुप्तों का आदि सम्बन्ध इस भाग से, बंगाल अथवा मगध की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे ढंग से सिद्ध किया जा सकता है । यह बात इस तरह देखने को मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्तों का मूल निवास-स्थान इसी भाग में रहा होगा ।
उस समय किन्तु इस मत के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुप्तों के लेख सबसे पहले चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम के समय से ही मिलते हैं । यह देखा गया था कि प्रारम्भिक काल का कोई लेख इस भाग से प्राप्त नहीं होता । यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त, रामगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के अधिकांश लेख पूर्वी मालवा क्षेत्र से मिले हैं । यह देखने को मिलता है कि जहाँ तक प्रयाग प्रशस्ति का प्रश्न है यह एक अशोक-स्तम्भ है जो मूलतः कौशाम्बी में गड़वाया गया था और कालान्तर में इसी के ऊपर समुद्रगुप्त ने अपना शेख अंकित करवा दिया । इस बात से यह संदेश मिलता है कि इसके आधार पर गुप्तों के मूल स्थान की समस्या हल नहीं की जा सकती । यह उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार उत्पत्ति के ही समान गुप्तों के मूल निवास स्थान का प्रश्न भी स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में विवाद का विषय बना हुआ है ।
गुप्त वंश की राजधानी क्या थी?
गुप्त वंश की राजधानीपाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार राज्य की राजधानी है और इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। प्राचीनकाल में पटना भारत एक सबसे बड़े महानगरों में से एक था। तब बिहार राज्य को मगध के नाम से जाना जता था।
Gupta Dynasty in Hindi: गुप्ता वंश के शासक (गुप्त वंश)
श्रीगुप्त
गुप्त वंश के पहले राजा का नाम श्रीगुप्त बताया जाता है।
घटोत्कच
घटोत्कच के बाद उसका पुत्र श्रीगुप्त शासक बना।
चन्द्रगुप्त प्रथम
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवि राजकुमारी से विवाह किया। प्रोफेसर आर एस शर्मा के अनुसार गुप्त शासक वैश्य (बनिया) थे और क्षत्रिय कुल में विवाह के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई।
समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक अद्वितीय शक्ति के रूप में भारत के अधिकांश लोगों का राजनीतिक एकीकरण था। समुद्रगुप्त ने महा राजाधिराज की उपाधि ली। सारे बड़े युद्ध जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ या अश्व यज्ञ किया। विदेशी राज्यों के कई शासकों जैसे शक और कुषाण राजाओं ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार किया और उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान कीं।
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त ने एक आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई। उन्होंने 375 से 415 ई तक शासन किया। उन्होंने शक-क्षत्रप वंश के रुद्रसिंह तृतीय को हराया और गुजरात में अपना साम्राज्य कायम किया।
कुमारगुप्त प्रथम
कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय से 451 ई में सत्ता प्राप्त की, और 450 ई तक 40 वर्षों की लंबी अवधि तक शासन किया। उनका शासन शांतिपूर्ण था।
स्कंदगुप्त
उसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की और 455ई से 467ई तक 12 वर्षों तक शासन किया। उसने हूणों को पराजित किया।
आशा करते हैं कि आपको Gupta Dynasty in Hindi ब्लॉग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी जितना हो सके अपने दोस्तों और बाकी सब को शेयर करें ताकि वह भी Gupta dynasty in Hindi के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे Leverage Edu में आपको इस प्रकार के बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे जहां आप अलग-अलग विषय में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो हमारे विशेषज्ञों आपकी सहायता भी करेंगे।
-
Very nice work
-
धन्यवाद
-
Wow bahut hi achcha explain kiya h tnxx
-
आपका आभार, ऐसे ही हमारी वेबसाइट पर बने रहिए।
-
-
-
-
Thanks

 One app for all your study abroad needs
One app for all your study abroad needs
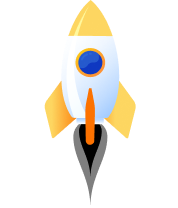


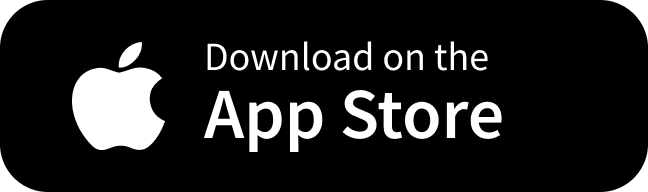











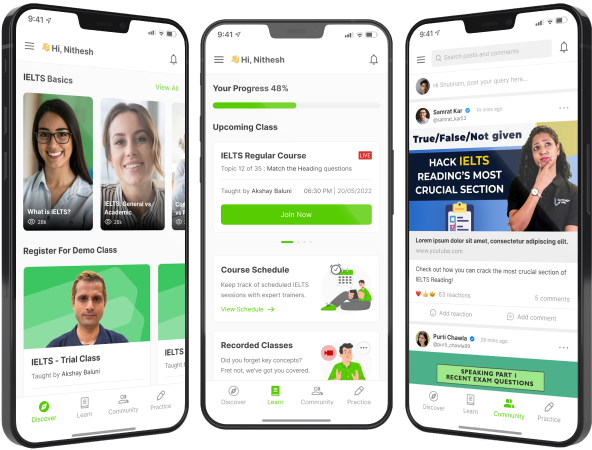



 45,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today.
45,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today.


5 comments
Very nice work
धन्यवाद
Wow bahut hi achcha explain kiya h tnxx
आपका आभार, ऐसे ही हमारी वेबसाइट पर बने रहिए।
Thanks